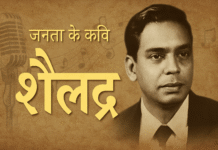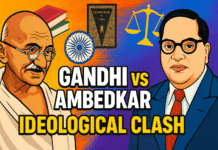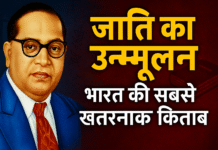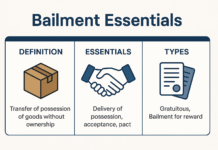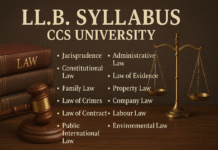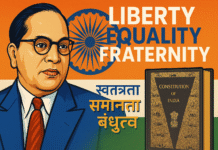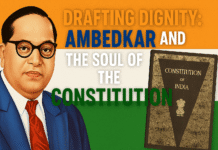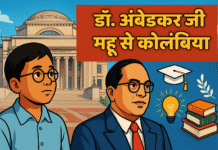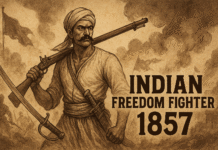जाति का उन्मूलन: क्या आज भी भारत की सबसे खतरनाक किताब है? – अम्बेडकर के क्रांतिकारी घोषणापत्र की गहरी पड़ताल
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की “जाति का उन्मूलन” भारतीय बौद्धिक इतिहास की सबसे विस्फोटक और परिवर्तनकारी रचनाओं में से एक है, जो प्रकाशन के लगभग नौ दशक बाद भी रूढ़िवादी हिंदू समाज, धार्मिक सत्ता और जाति-आधारित सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देती रहती है। मूल रूप से 1936 में जाट-पाट तोड़क मंडल के लिए भाषण के रूप में लिखी गई यह रचना इतनी विवादास्पद मानी गई कि इसे दिया ही नहीं जा सका, लेकिन यह सामाजिक क्रांति का घोषणापत्र बन गई जो आज भी स्थापित शक्ति संरचनाओं को धमकाती है। हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद की इसकी कट्टर आलोचना, सुधार के बजाय जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान, और निरंतर जाति हिंसा के सामने इसकी समसामयिक प्रासंगिकता इसे पहले से कहीं अधिक खतरनाक बनाती है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2022 में अनुसूचित जातियों पर 57,000 से अधिक अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही साप्ताहिक रूप से मैनुअल स्कैवेंजिंग की मौतें हो रही हैं, जो दिखाता है कि जाति उत्पीड़न की निरंतरता के बारे में अम्बेडकर की चेतावनियां आज भी डरावनी रूप से सटीक हैं। [1]
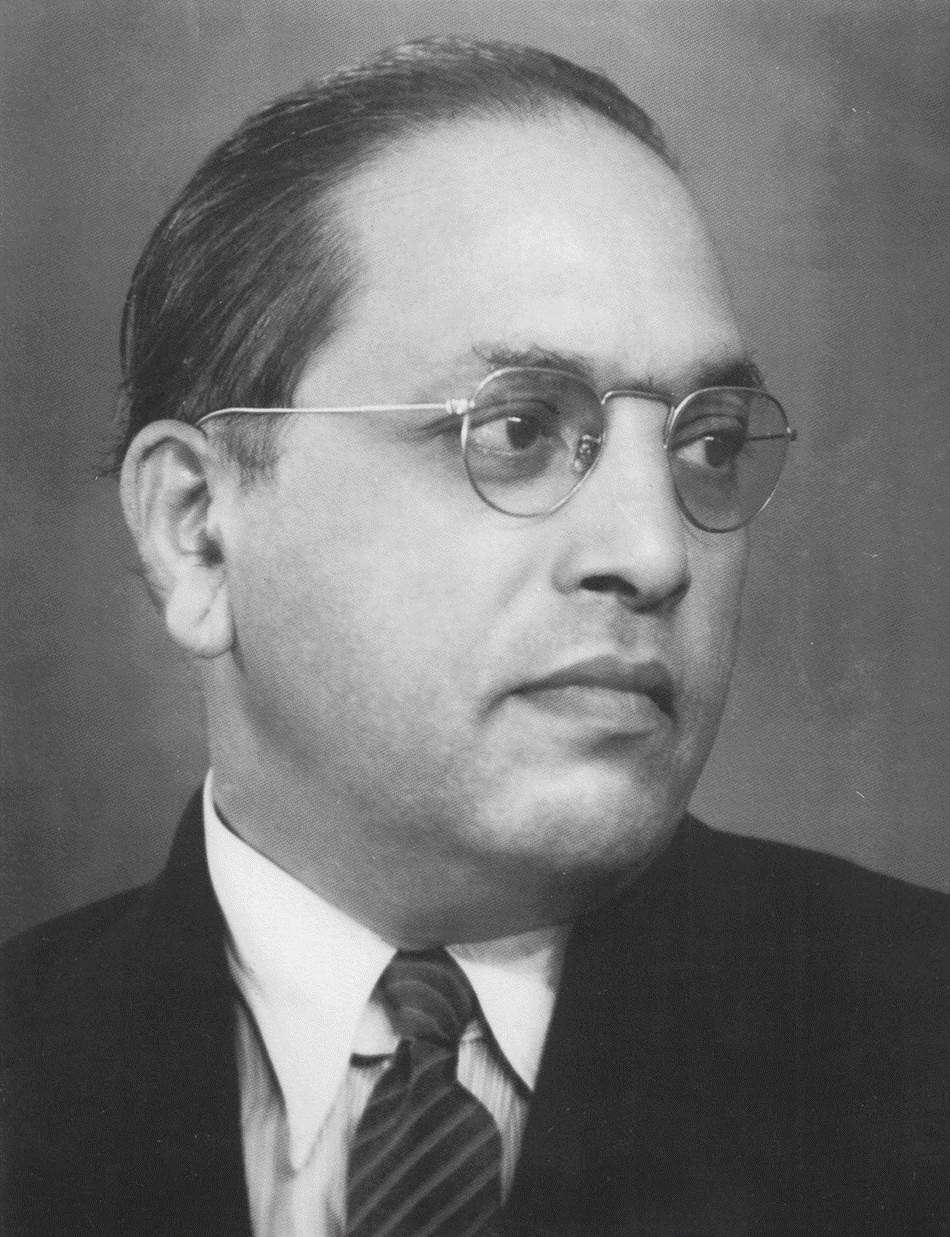
Formal historical portrait of B. R. Ambedkar, author of Annihilation of Caste and prominent Indian social reformer.
ऐतिहासिक संदर्भ और वह विवाद जो कभी पहुंचाया ही नहीं गया
“जाति का उन्मूलन” की उत्पत्ति से ही पता चलता है कि शुरू से ही इसे बहुत खतरनाक क्यों माना गया था। दिसंबर 1935 में लाहौर स्थित एक हिंदू सुधारवादी संगठन जाट-पाट तोड़क मंडल ने डॉ. अम्बेडकर को जाति व्यवस्था पर अपने वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन जब आयोजकों ने अम्बेडकर के तैयार किए गए पाठ की समीक्षा की, तो उन्होंने पाया कि यह “रूढ़िवादी हिंदू धर्म के प्रति इतना आपत्तिजनक” और “हिंदू धर्म से दूर धर्मांतरण को बढ़ावा देने में इतना भड़काऊ” था कि उन्होंने इसमें बड़े बदलाव की मांग की। इस सामग्री को न केवल विवादास्पद बल्कि उन सुधारवादियों द्वारा “असहनीय” माना गया जिन्होंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया था। [2]
अम्बेडकर की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अडिग थी: उन्होंने घोषणा की कि वे अपने पाठ से “एक कॉमा भी नहीं बदलेंगे”। समझौता करने से इस इनकार ने आयोजकों को अपना पूरा वार्षिक सम्मेलन रद्द करने पर मजबूर कर दिया, बजाय इसके कि वे उस हिंसा का जोखिम उठाते जिसके वे डरते थे कि अगर भाषण लिखे गए रूप में दिया जाता तो रूढ़िवादी हिंदू कर सकते थे। रद्दीकरण ने ही अम्बेडकर के विचारों की विस्फोटक प्रकृति को दिखा दिया – यहां तक कि प्रगतिशील हिंदू सुधारक भी उनकी धार्मिक नींव की पूर्ण अस्वीकृति को पचा नहीं सकते थे। [3][2]
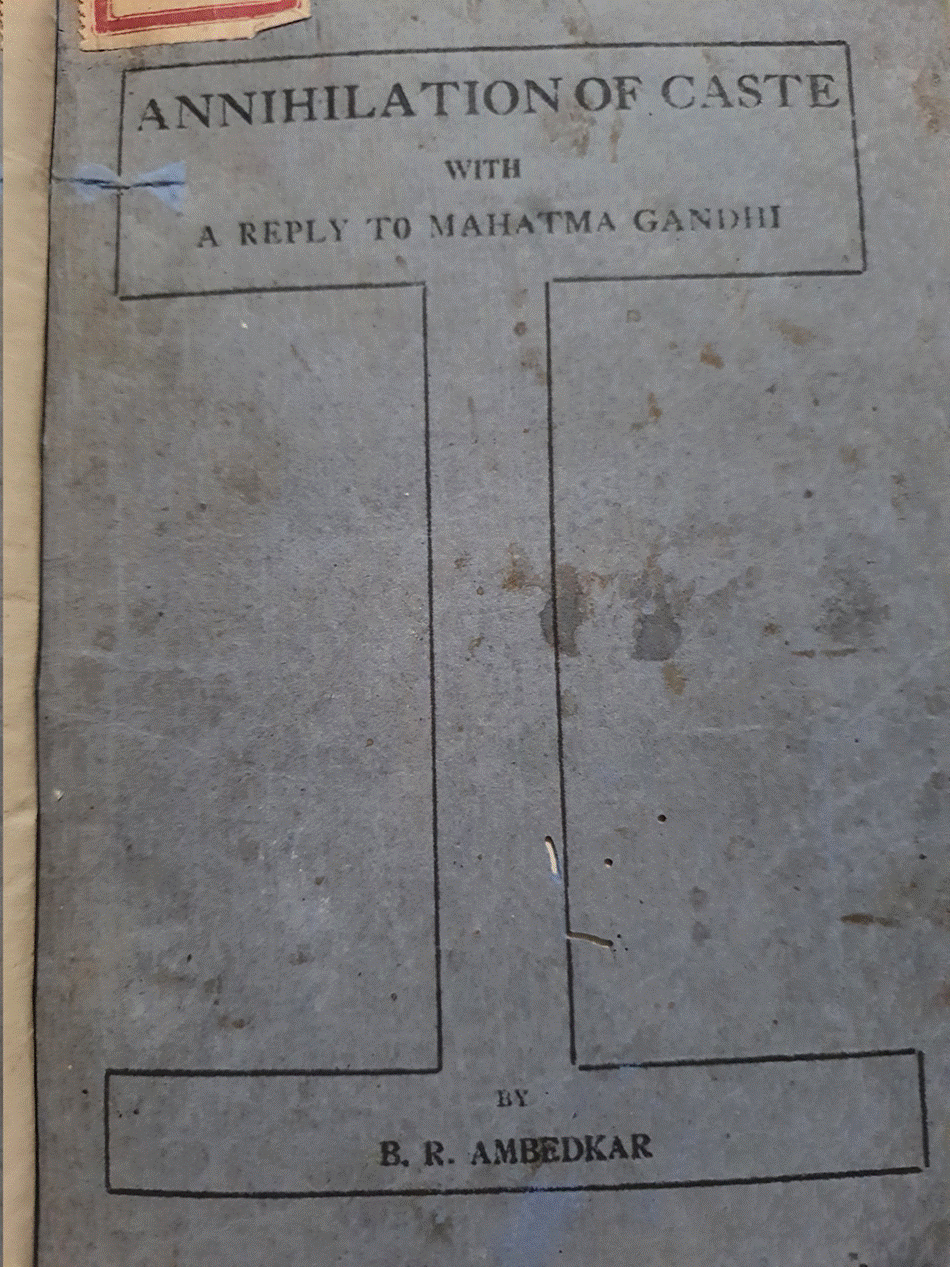
Cover page of B. R. Ambedkar’s seminal book “Annihilation of Caste” featuring a reply to Mahatma Gandhi.
इस अस्वीकृति से निराश न होकर, अम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपने खर्चे पर भाषण की 1,500 प्रतियां स्वयं प्रकाशित कीं। पुस्तक का तत्काल प्रभाव गहरा था, जिसने कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद को प्रेरित किया और हिंदू समाज की सबसे प्रभावशाली आलोचनाओं में से एक स्थापित की जो कभी लिखी गई थी। इसकी गैर-डिलीवरी के आसपास का विवाद वास्तव में इसके संदेश को बढ़ाता गया, एक अस्वीकृत भाषण को एक क्रांतिकारी घोषणापत्र में बदल दिया जो आज भी भारतीय समाज को चुनौती देता रहता है। [2]
खतरे का विश्लेषण: अम्बेडकर के कट्टरपंथी तर्क
धार्मिक सत्ता की पूर्ण अस्वीकृति
“जाति का उन्मूलन” को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली बात अम्बेडकर की हिंदू शास्त्रीय सत्ता की पूर्ण अस्वीकृति है। अन्य सुधारकों के विपरीत जो धार्मिक ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करना चाहते थे, अम्बेडकर ने उन्हें पूरी तरह से त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि “जाति को नष्ट करने की वास्तविक कुंजी शास्त्रों की अस्वीकृति है” और “शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास” को सच्चे सामाजिक परिवर्तन के लिए नष्ट करना होगा। हिंदू धर्म की धार्मिक नींव पर यह प्रत्यक्ष हमला रूढ़िवादी विश्वास प्रणालियों के बहुत मूल पर प्रहार करता था। [4][5]
अम्बेडकर की आलोचना व्यक्तिगत ग्रंथों से आगे बढ़कर धार्मिक अचूकता की पूरी अवधारणा को चुनौती देती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे ऐसे ग्रंथ जो “समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अमानवीय बनाते हैं, नैतिक वैधता का दावा कर सकते हैं” और तर्क दिया कि मनुस्मृति जैसे हिंदू ग्रंथ “स्पष्ट रूप से जाति पदानुक्रम को संहिताबद्ध करते हैं”। 1927 में मनुस्मृति को उनका सार्वजनिक जलाना उस बौद्धिक हमले का प्रतीकात्मक कार्य था जो वे “जाति का उन्मूलन” में शुरू करेंगे। [6][7]
इस दृष्टिकोण का खतरा तब स्पष्ट हो जाता है जब अन्य समसामयिक सुधारकों के साथ तुलना की जाती है। जबकि महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व अस्पृश्यता को समाप्त करते हुए हिंदू धर्म को संरक्षित करना चाहते थे, अम्बेडकर ने तर्क दिया कि यह असंभव था। उन्होंने दावा किया कि जाति हिंदू धार्मिक सिद्धांत का इतना अभिन्न अंग था कि भीतर से सुधार निरर्थक था – केवल धार्मिक आधार की पूर्ण अस्वीकृति ही सच्ची समानता हासिल कर सकती थी। [8][9][4][6]
जाति औचित्य का व्यवस्थित विध्वंस
अम्बेडकर के पाठ ने जाति व्यवस्था के हर प्रमुख औचित्य को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया, समझौते या क्रमिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने इस तर्क को खारिज किया कि जाति “श्रम विभाजन” का प्राकृतिक प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि तर्क दिया कि यह “श्रमिकों का विभाजन” था जो लोगों को उनकी क्षमताओं या झुकाव की परवाह किए बिना वंशानुगत व्यवसायों में फंसाता था। यह भेद महत्वपूर्ण था – इसने जाति को एक कुशल सामाजिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक दमनकारी व्यवस्था के रूप में उजागर किया जो दूसरों की कीमत पर ऊपरी जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। [4][9][10][11]
आर्थिक आलोचना भी उतनी ही विनाशकारी थी। अम्बेडकर ने दिखाया कि “जाति का परिणाम आर्थिक दक्षता में नहीं होता” और व्यावसायिक गतिशीलता को रोकर, यह “बेरोजगारी और अविकसितता का प्रत्यक्ष कारण” बन गया। उन्होंने दिखाया कि यह व्यवस्था निचली जातियों से बुनियादी आर्थिक अधिकार छीनती है, दलितों के लिए जो “शिक्षा और व्यवसाय की स्वतंत्रता से वंचित हैं”, “आर्थिक गुलामी” का निर्माण करती है। [12][13]
शायद सबसे खतरनाक रूप से, अम्बेडकर ने जाति की “असामाजिक भावना” को उजागर किया, यह तर्क देते हुए कि यह वास्तविक राष्ट्रीय एकता के गठन को रोकती है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू समाज बिल्कुल भी एक समाज नहीं था बल्कि केवल “जातियों का संग्रह था, जिनके अपने असामाजिक जाति हित थे”। इस विश्लेषण ने सीधे राष्ट्रवादी कथाओं को चुनौती दी जो आंतरिक विभाजनों को अनदेखा करते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करना चाहती थीं। [14][12]
विवाह समाधान और इसके कट्टरपंथी निहितार्थ
“जाति का उन्मूलन” के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक अम्बेडकर द्वारा अंतर-जातीय विवाह को जाति विभाजन के प्राथमिक समाधान के रूप में पहचान करना था। उन्होंने तर्क दिया कि “जाति तोड़ने का वास्तविक उपाय अंतर-विवाह है। जाति के विलायक के रूप में कुछ और काम नहीं करेगा”। यह केवल एक सामाजिक सुझाव नहीं था बल्कि एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था जो जाति रखरखाव के दिल पर प्रहार करता था। [15][16]
अम्बेडकर समझते थे कि अंतर्विवाह – अपनी ही जाति के भीतर विवाह – “जाति का सार” था और “जाति व्यवस्था की महारत की कुंजी” था। अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से इसके पूर्ण परित्याग का आह्वान करके, वे उस प्राथमिक तंत्र के विनाश का प्रस्ताव कर रहे थे जो जातियों को अलग और पदानुक्रमित रखता था। उन्होंने माना कि “रक्त का संलयन ही रिश्तेदार और नातेदार होने की भावना पैदा कर सकता है” और इसके बिना “अलगाववादी भावना-पराए होने की भावना-जाति द्वारा बनाई गई गायब नहीं होगी”। [16][17][15]
यह प्रस्ताव आज भी खतरनाक है क्योंकि अंतर-जातीय विवाह अभी भी भारत में सभी विवाहों का केवल लगभग 6% हैं और हिंसक विरोध का सामना करते रहते हैं। ऑनर किलिंग, पारिवारिक बहिष्कार, और अंतर-जातीय जोड़ों के खिलाफ सामुदायिक हिंसा दिखाती है कि अम्बेडकर का समाधान रूढ़िवादी समाज के लिए उतना ही खतरनाक है जितना 1936 में था। [18][19][20]
गांधी-अम्बेडकर बहस: मौलिक दार्शनिक विभाजन
“जाति का उन्मूलन” पर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच बौद्धिक युद्ध ने भारतीय सामाजिक चिंतन में सुधार और क्रांति के बीच मौलिक विभाजन को उजागर किया। जब गांधी ने अपने अखबार हरिजन में काम की समीक्षा की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि “कोई भी सुधारवादी इस भाषण को नजरअंदाज नहीं कर सकता” लेकिन अम्बेडकर को “हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती” बताया। यह चरित्र-चित्रण शायद गांधी के इरादे से कहीं अधिक सटीक था – अम्बेडकर वास्तव में पारंपरिक रूप से कल्पना किए गए हिंदू धर्म के अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे। [3][8][21]
गांधी का दृष्टिकोण अस्पृश्यता को समाप्त करते हुए वर्ण व्यवस्था को संरक्षित करना चाहता था, यह मानते हुए कि हिंदू धर्म को भीतर से सुधारा जा सकता है। उन्होंने योग्यता पर आधारित एक “आदर्शीकृत वर्ण” और भ्रष्ट जाति व्यवस्था के बीच अंतर किया, यह तर्क देते हुए कि अगर ठीक से लागू किया जाए तो पूर्व सामाजिक सद्भावना प्रदान कर सकता है। गांधी की रणनीति सुधार प्राप्त करने के लिए मौजूदा धार्मिक ढांचे के भीतर काम करते हुए नैतिक अनुनय और क्रमिक परिवर्तन पर निर्भर थी। [8][9][22]
अम्बेडकर की प्रतिक्रिया अपनी स्पष्टता में विनाशकारी थी। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण और जाति अविभाज्य हैं, पदानुक्रम को पवित्र बनाने वाले धार्मिक ग्रंथों की चुनिंदा व्याख्या नहीं की जा सकती, और क्रमिक सुधार सदियों से असफल रहा है। रूढ़िवादी हितों के लिए सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने दिखाया कि गांधी का दृष्टिकोण उन्हीं नींवों को संरक्षित करेगा जो जाति उत्पीड़न को जारी रखने में सक्षम बनाती हैं। उन्होंने गांधी की आलोचना का एक लंबा जवाब लिखा, “गांधी की अंधविश्वासी और तर्कहीन मान्यताओं को रेखांकित करते हुए” और यह तर्क देते हुए कि “हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है और इसे टालना खतरनाक होगा”। [6][9][3]
यह बहस आज भी प्रासंगिक है क्योंकि जाति असमानता को संबोधित करने के विभिन्न दृष्टिकोण भारतीय समाज को विभाजित करते रहते हैं। मूलभूत असमानताओं को बरकरार रखते हुए प्रतीकात्मक इशारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले समसामयिक प्रयासों को सतही सुधार के बजाय संरचनात्मक परिवर्तन पर अम्बेडकर का आग्रह चुनौती देता है। [23]
समसामयिक प्रासंगिकता: आज भी किताब खतरनाक क्यों है
निरंतर जाति हिंसा और भेदभाव
“जाति का उन्मूलन” की समसामयिक प्रासंगिकता दुखद रूप से जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव के निरंतर आंकड़ों से प्रदर्शित होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों के लिए 57,582 मामले दर्ज किए गए, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसे अम्बेडकर ने जाति प्रथा के सबसे अमानवीय पहलुओं में से एक के रूप में पहचाना था, साप्ताहिक रूप से जीवन लेती रहती है, लगभग हर सप्ताह सेप्टिक टैंक में एक मैनुअल स्कैवेंजर की मृत्यु हो जाती है। [1][19]
भारत भर की हाल की घटनाएं इस बात की स्थायी खतरनाक प्रकृति को दर्शाती हैं जो अम्बेडकर के विचार स्थापित शक्ति संरचनाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक, दलित बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने के लिए हिंसा का सामना करते रहते हैं – ऊंची जाति के स्रोतों से पानी पीना, अम्बेडकर जयंती मनाना, या केवल अच्छे कपड़े पहनना। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अम्बेडकर द्वारा पहचानी गई “सामाजिक अत्याचार” जो राजनीतिक अत्याचार से अधिक दमनकारी है, लाखों भारतीयों के लिए एक जीवंत वास्तविकता बनी हुई है। [19][20]
शैक्षणिक आंकड़े भी उतने ही निंदनीय हैं। संवैधानिक सुरक्षा और आरक्षण नीतियों के बावजूद, 71.3% अनुसूचित जाति के छात्र मैट्रिक से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि बुनियादी सरकारी नौकरी आरक्षण भी केवल चार में से एक दलित पर लागू होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार दलित जनसंख्या का केवल 2.24% ही स्नातक है, यह आंकड़ा बाद के दशकों में केवल मामूली रूप से सुधरा है। [24]
राजनीतिक दुरुपयोग और प्रतिरोध
रूढ़िवादी हितों के लिए शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि “जाति का उन्मूलन” समकालीन प्रतिरोध आंदोलनों के लिए एक आधारशिला बन गया है। राजनीतिक नेता चुनावी अभियानों के दौरान अम्बेडकर और संविधान का तेजी से आह्वान करते हैं, हालांकि अक्सर हिंदू समाज की उनकी कट्टरपंथी आलोचना को स्वीकार किए बिना। जैसा कि दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सूरज येंगड़े देखते हैं, “अम्बेडकर की छवि का उपयोग किसी भी मुद्दे के आसपास दलित गुस्से को शांत करने के लिए किया जाता है, उत्पीड़क के फायदे के लिए, जो अम्बेडकर को अपने घृणा और हिंसा के दुष्ट कार्यक्रम में शामिल करने में खुशी से अधिक है”। [1]
हिंदुत्व राजनीति के उदय ने “हिंदू राज” के बारे में अम्बेडकर की चेतावनियों को विशेष तात्कालिकता दी है। 1940 के दशक में, उन्होंने चेतावनी दी थी कि “यदि हिंदू राज एक वास्तविकता बन जाता है, तो यह निस्संदेह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हिंदू जो कुछ भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। यह लोकतंत्र के साथ असंगत है”। समकालीन विद्वानों का तर्क है कि यह चेतावनी भविष्यवाणी साबित हुई है, क्योंकि आरएसएस और संबद्ध संगठनों ने “भारतीय समाज के पूरे मैक्रो और माइक्रो स्पेसेस पर कड़ी पकड़” स्थापित की है जबकि मनुस्मृति-आधारित विचारधारा को बढ़ावा देते हैं जो “दलितों और महिलाओं को मानव से कम मानती है”। [7]
डिजिटल युग की अभिव्यक्तियां
डिजिटल युग ने उन खतरों को नए आयाम दिए हैं जो “जाति का उन्मूलन” रूढ़िवादी समाज के लिए प्रस्तुत करता है। जाति भेदभाव ऑनलाइन चला गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाति-आधारित उत्पीड़न और बहिष्कार के स्थान बन गए हैं। डेटिंग ऐप्स जाति के आधार पर फ़िल्टरिंग की रिपोर्ट करते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में कार्यस्थल भेदभाव जारी रहता है, और यहां तक कि सिलिकॉन वैली में भी भारतीय पेशेवरों के बीच जाति-आधारित भेदभाव देखा गया है।[7][25]
साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अम्बेडकर के लेखन तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है, “जाति का उन्मूलन” को उन पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है जो शायद पारंपरिक शैक्षणिक प्रणालियों के माध्यम से इसका सामना कभी नहीं करते। ऑनलाइन चर्चा, सोशल मीडिया अभियान, और डिजिटल सक्रियता ने पाठ की पहुंच को बढ़ाया है, इसके कट्टरपंथी संदेश को पाठकों की नई पीढ़ियों के लिए उपलब्ध कराया है जो इसका उपयोग जाति उत्पीड़न की समकालीन अभिव्यक्तियों को चुनौती देने के लिए करते हैं।
अधूरी क्रांति: शैक्षणिक और कानूनी निहितार्थ
आक्रमण के तहत आरक्षण नीतियां
अम्बेडकर के संवैधानिक ढांचे से उभरी आरक्षण प्रणाली उन चुनौतियों का सामना करती रहती है जो दिखाती हैं कि “जाति का उन्मूलन” रूढ़िवादी हितों के लिए खतरनाक क्यों रहता है। 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण की शुरुआत को आलोचकों द्वारा जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली को कमजोर करने के रूप में देखा गया है जिसे अम्बेडकर ने डिज़ाइन किया था। जाति-आधारित मानदंडों के बजाय आर्थिक मानदंडों की ओर यह कदम उन बहसों की गूंज है जिन्हें अम्बेडकर ने 1936 में जाति उत्पीड़न की मौलिक प्रकृति के बारे में संबोधित किया था। [7]
आरक्षण नीतियों की समकालीन आलोचना अक्सर उन्हीं तर्कों को दर्शाती है जिन्हें अम्बेडकर ने 1936 में ध्वस्त किया था। दावे कि आरक्षण “योग्यता” और “शिक्षा की गुणवत्ता” को प्रभावित करते हैं, उसी तर्क की गूंज हैं जो पारंपरिक व्यवसायों में जाति-आधारित बहिष्कार को संरक्षित करने की मांग करते थे। आईआईटी और आईआईएम जैसे अभिजात्य संस्थानों में जाति-आधारित आरक्षण का प्रतिरोध दिखाता है कि “बौद्धिक वर्ग” अम्बेडकर द्वारा आलोचित – जिसे उन्होंने तर्क दिया था “केवल ब्राह्मण जाति का दूसरा नाम है” – उन संरचनात्मक परिवर्तनों का विरोध करते रहते हैं जो उनके प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। [26][27]
संवैधानिक लोकतंत्र बनाम सामाजिक पदानुक्रम
अम्बेडकर की प्रसिद्ध चेतावनी कि “लोकतंत्र केवल भारतीय मिट्टी पर एक ऊपरी ड्रेसिंग है जो मूल रूप से अलोकतांत्रिक है” ने समकालीन भारत में नई प्रासंगिकता हासिल की है। समानता की संवैधानिक गारंटी और जाति पदानुक्रम की जीवित वास्तविकता के बीच का विरोधाभास उन तनावों को उत्पन्न करता रहता है जिनकी अम्बेडकर ने भविष्यवाणी की थी। उनका अवलोकन कि “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र न हो” भारतीय समाज के लिए एक मौलिक चुनौती बनी हुई है। [1]
लोकतांत्रिक अधिकारों के दावे के लिए दलितों की मृत्यु – जिसे विद्वान जदुमणि महानंद “जाति द्वारा मृत्यु” कहते हैं – अम्बेडकर के विश्लेषण की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है। चाहे प्रत्यक्ष हिंसा के माध्यम से या मैनुअल स्कैवेंजिंग की अप्रत्यक्ष हिंसा के माध्यम से, “मनु के कानून” सामाजिक शक्ति को नियंत्रित करते रहते हैं जो “भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ लड़ता है”। संवैधानिक कानून और सामाजिक रिवाज के बीच यह तनाव अम्बेडकर के मूल पाठ की क्रांतिकारी क्षमता को बनाए रखता है। [19]
वैश्विक कनेक्शन और सार्वभौमिक प्रासंगिकता
“जाति का उन्मूलन” ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है क्योंकि व्यवस्थित उत्पीड़न का इसका विश्लेषण भेदभाव के खिलाफ वैश्विक संघर्षों के साथ गूंजता है। अफ्रीकी-अमेरिकी बौद्धिक डब्ल्यू.ई.बी. डू बॉइस के साथ अम्बेडकर के पत्राचार में, जहां उन्होंने “भारत में अछूतों की स्थिति और अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों की स्थिति के बीच बहुत समानता” देखी, ने जाति-विरोधी आंदोलनों और अन्य सामाजिक न्याय संघर्षों के बीच संबंध स्थापित किए। [1][11]
समकालीन विद्वानों ने जाति भेदभाव और अन्य व्यवस्थित उत्पीड़न के रूपों के बीच समानताएं खींची हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शामिल है। इन वैश्विक कनेक्शनों ने पाठ के प्रभाव को मजबूत किया है जबकि इसे स्थापित हितों के लिए और भी खतरनाक बनाया है, क्योंकि यह कई प्रकार की व्यवस्थित असमानता को समझने और चुनौती देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। [11]
काम का प्रभाव शैक्षणिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक न्याय, और विभिन्न राष्ट्रीय संदर्भों में संरचनात्मक असमानता के बारे में व्यावहारिक नीति चर्चाओं तक पहुंचता है। दमनकारी प्रणालियां धार्मिक स्वीकृति, सामाजिक रिवाज, और आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से खुद को कैसे बनाए रखती हैं, इसका इसका व्यवस्थित विश्लेषण विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित भेदभाव के खिलाफ संघर्षों पर लागू अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
पुस्तक “खतरनाक” क्यों रहती है
धार्मिक रूढ़िवादी सत्ता के लिए खतरा
“जाति का उन्मूलन” खतरनाक रहती है क्योंकि यह हिंदू समाज में धार्मिक रूढ़िवादी सत्ता के लिए एक मौलिक खतरा बनी हुई है। न केवल विशिष्ट प्रथाओं बल्कि जाति पदानुक्रम को न्यायसंगत बनाने वाली पूरी शास्त्रीय नींव पर सवाल उठाकर, पाठ पारंपरिक धार्मिक नेतृत्व की वैधता को चुनौती देता है। “शास्त्रों के दिव्य अधिकार को छोड़ने” के लिए अम्बेडकर का आह्वान आज भी उतना ही कट्टरपंथी है जितना 1936 में था, विशेष रूप से हिंदुत्व राजनीति धार्मिक रूढ़िवाद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। [4][7]
पाठ का खतरा धार्मिक तर्कों को ध्वस्त करने के लिए इसके तर्कसंगत, व्यवस्थित दृष्टिकोण से और बढ़ता है। पवित्र ग्रंथों की वैकल्पिक व्याख्याओं की पेशकश करने के बजाय, अम्बेडकर मानव समानता और गरिमा के साथ उनकी मौलिक असंगति प्रदर्शित करते हैं। यह दृष्टिकोण काम को उस प्रकार के चुनिंदा उद्धरण और पुनर्व्याख्या से प्रतिरक्षित बनाता है जिसका उपयोग रूढ़िवादी ताकतें अक्सर सुधार आंदोलनों को निष्क्रिय करने के लिए करती हैं।
समकालीन शक्ति संरचनाओं के लिए चुनौती
“श्रेणीबद्ध असमानता” की व्यवस्था के रूप में जाति कैसे कार्य करती है, इसकी पुस्तक का विश्लेषण समकालीन शक्ति संरचनाओं के लिए खतरनाक रूप से प्रासंगिक रहता है। अम्बेडकर की पहचान कि जाति केवल सांस्कृतिक अंतर नहीं बल्कि व्यवस्थित आर्थिक शोषण है, रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ऊपरी जातियों को फायदा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं को धमकाती रहती है। “आर्थिक गुलामी” बनाने के उनके तर्क समकालीन विश्लेषणों के साथ शक्तिशाली रूप से गूंजते हैं धन असमानता और अवसर की पहुंच का।
संरचनात्मक के बजाय सतही परिवर्तन के लिए पाठ का आह्वान समकालीन दृष्टिकोणों को चुनौती देता है जो मौलिक शक्ति संबंधों को बरकरार रखते हुए सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण, विविधता पहल, या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अम्बेडकर का आग्रह कि “आर्थिक सुधारों के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है” और संरचनात्मक परिवर्तन के बिना, यहां तक कि राजनीतिक क्रांति भी असफल हो जाएगी, सीधे उन दृष्टिकोणों का विरोध करता है जो जाति को व्यवस्थित उत्पीड़न के बजाय केवल सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में मानते हैं।
निरंतर प्रतिरोध के लिए प्रेरणा
स्थापित हितों के लिए शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि “जाति का उन्मूलन” जाति-विरोधी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। पाठ व्यवस्थित उत्पीड़न को समझने के लिए दोनों विश्लेषणात्मक उपकरण और इसे खत्म करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। “जाति के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा और जागरूकता के महत्व” पर अम्बेडकर का जोर उत्पीड़ित समुदायों के बीच शैक्षणिक पहुंच और आलोचनात्मक चेतना के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया है।[11]
समकालीन दलित साहित्य, सक्रियता और राजनीतिक आंदोलनों पर काम का प्रभाव प्रतिरोध को संगठित करने की इसकी निरंतर शक्ति को प्रदर्शित करता है। शैक्षणिक सम्मेलनों से सड़क प्रदर्शनों तक, कानूनी चुनौतियों से सांस्कृतिक आंदोलनों तक, “जाति का उन्मूलन” जाति उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह लगभग नौ दशक पहले था।

Protesters rally near a statue of Dr. B.R. Ambedkar, championing Dalit rights and caste equality in India.
निष्कर्ष: निरंतर क्रांति
“जाति का उन्मूलन” भारत की सबसे खतरनाक पुस्तक इसीलिए रहती है क्योंकि इसकी कल्पना की गई क्रांति अधूरी रहती है। हिंदू रूढ़िवाद की अम्बेडकर की व्यवस्थित आलोचना, क्रमिक सुधार के बजाय पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का उनका आह्वान, और “स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे” पर आधारित समाज का उनका दृष्टिकोण भारतीय समाज में स्थापित शक्ति संरचनाओं के लिए मौलिक चुनौतियां पेश करते रहते हैं। जाति हिंसा की निरंतरता, संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतिरोध, और उनके कट्टरपंथी संदेश को नजरअंदाज करते हुए अम्बेडकर की छवि का दुरुपयोग सभी दिखाते हैं कि यह पाठ आज भी उतना ही खतरनाक क्यों है जितना 1936 में था जब रूढ़िवादी हिंदू सुधारकों ने इसे दिए जाने से मना कर दिया था।
पुस्तक की समसामयिक प्रासंगिकता दुखद रूप से अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के 57,000 से अधिक वार्षिक मामलों, मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतर प्रथा, और अंतर-जातीय विवाहों के हिंसक विरोध को दिखाने वाले आंकड़ों से पुष्ट होती है। ये वास्तविकताएं दिखाती हैं कि धार्मिक रूढ़िवाद द्वारा पवित्र की गई व्यवस्थित उत्पीड़न की व्यवस्था के रूप में जाति का अम्बेडकर का विश्लेषण विनाशकारी रूप से सटीक रहता है। उनकी चेतावनी कि क्रमिक सुधार मौलिक असमानताओं को संबोधित करने में असफल होगा, भविष्यवाणी साबित हुई है, क्योंकि दशकों की संवैधानिक सुरक्षा और कानूनी उपचार “सामाजिक अत्याचार” को खत्म करने में असफल रहे हैं जिसे उन्होंने राजनीतिक उत्पीड़न से अधिक दमनकारी के रूप में पहचाना था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि “जाति का उन्मूलन” खतरनाक रहती है क्योंकि यह केवल आलोचना नहीं बल्कि वास्तविक परिवर्तन का रोडमैप प्रदान करती है। पदानुक्रम के औचित्य का इसका व्यवस्थित विध्वंस, अंतर-विवाह और शैक्षणिक पहुंच जैसे व्यावहारिक समाधानों की इसकी पहचान, और पारंपरिक प्राधिकरण को स्वीकार करने के बजाय प्रश्न करने पर इसका आग्रह सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे युग में जहां प्रतीकात्मक इशारे अक्सर संरचनात्मक परिवर्तन का स्थान लेते हैं, पूर्ण सामाजिक परिवर्तन का अम्बेडकर का अनुपम दृष्टिकोण एक खतरनाक अनुस्मारक है कि वास्तविक समानता की क्या आवश्यकता होगी।
पाठ की स्थायी शक्ति इसके ऐतिहासिक महत्व में नहीं बल्कि इसकी समसामयिक तात्कालिकता में निहित है। जैसे-जैसे भारत बढ़ती असमानता, धार्मिक रूढ़िवाद और व्यवस्थित भेदभाव से जूझता है, “जाति का उन्मूलन” नैदानिक उपकरण और निर्देशक समाधान दोनों प्रदान करता है जो आज भी उतने ही कट्टरपंथी हैं जितने वे लगभग एक सदी पहले क्रांतिकारी थे। यह खतरनाक इसलिए रहती है कि यह प्रासंगिक रहती है – और यह प्रासंगिक इसलिए रहती है कि इसकी कल्पना की गई क्रांति अभी तक हासिल नहीं हुई है।
- https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Apr/14/ambedkar-a-revolutionarys-vision-for-equality-continues-to-inspire-and-challenge-todays-india
- https://en.wikipedia.org/wiki/Annihilation_of_Caste
- https://www.forwardpress.in/2018/11/annihilation-of-caste-key-to-building-india/
- https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/75088/1/Unit-1.pdf
- https://indianhistorycollective.com/annihilation-by-babasaheb-part-2/
- https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2505765.pdf
- https://countercurrents.org/2025/04/commemorating-135th-birth-anniversary-of-ambedkar-the-biggest-ideological-enemy-of-rss/
- https://www.cvs.edu.in/upload/Ambedkar Gandhi Debate.pdf
- https://www.granthaalayahpublication.org/Arts-Journal/ShodhKosh/article/download/2381/2126/16987
- https://www.literarysphere.com/2024/02/summary-of-dr-ambedkars-annihilation-of.html
- https://voiceofresearch.org/Doc/Sep-2024/Sep-2024_3.pdf
- https://www.thecollector.com/hindu-caste-system-ambedkar/
- https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA/recent_issues_pdf/2015/July/July_2015_1437477848__167.pdf
- https://www.studocu.com/in/document/university-of-delhi/sociology-of-india-ii/annhiliation-of-caste/113458786
- https://www.roundtableindia.co.in/the-real-remedy-for-breaking-caste/
- https://thewire.in/politics/caste/on-ambedkar-jayanti-remembering-the-annihilation-of-caste
- https://chahalacademy.com/inter-caste-marriage
- https://smashboard.org/re-reading-ambedkars-insistence-on-inter-caste-marriages/
- https://www.theindiaforum.in/caste/death-dalit-democracy
- https://cjp.org.in/the-alarming-rise-of-anti-dalit-violence-and-discrimination-in-india-a-series-of-gruesome-incidents-since-july-2024/
- https://www.linkedin.com/pulse/great-debate-br-ambedkar-mahatma-gandhi-caste-sahil-sajad-ac6cc
- https://discoursereview.com/article/the-gandhi-ambedkar-caste-debates-a-critical-reading-of-the-varna-discourse/
- https://latest.sundayguardianlive.com/opinion/b-r-ambedkars-annihilation-of-caste-is-still-relevant
- https://ia601202.us.archive.org/23/items/AnnihilationOfCasteDr.B.r.ambedkar/Annihilation of caste Dr.B.r.ambedkar.pdf
- https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2455328X241266637?download=true
- https://businesseconomics.in/analysis-reservation-policy-indian-education-system
- https://kseliteattorneys.com/single_article.php?id=53