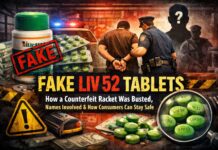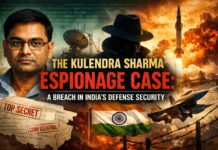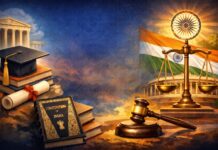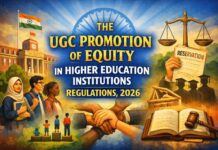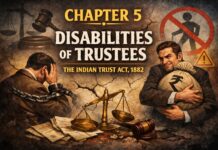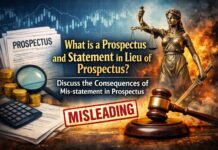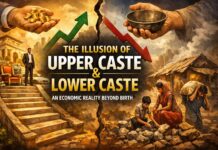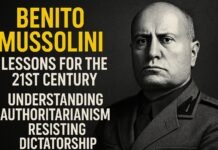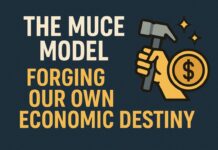जातिवादी पत्रकारिता और समाज पर इसके प्रभाव: भारत में मीडिया पूर्वाग्रह और सामाजिक न्याय का विश्लेषण
भारत का मीडिया जगत, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाने के बावजूद, जाति-आधारित पूर्वाग्रहों में गहराई से फंसा हुआ है। यह व्यवस्थित भेदभाव को बनाए रखता है और कमजोर समुदायों का हाशियाकरण करता है। यह व्यापक विश्लेषण दिखाता है कि कैसे जातिवादी पत्रकारिता—जाति की सुविधा के नजरिए से समाचार रिपोर्टिंग, फ्रेमिंग और प्रस्तुतीकरण की प्रथा—आज भी सार्वजनिक बहस को आकार देती है, सामाजिक कहानियों को प्रभावित करती है, और आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर डालती है।

जातिवादी पत्रकारिता को समझना
जातिवादी पत्रकारिता भारत के मीडिया ढांचे में संरचनात्मक भेदभाव की एक जटिल अभिव्यक्ति है, जहां समाचार उत्पादन, संपादकीय निर्णय, और कहानी निर्माण जाति-आधारित पदानुक्रम और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यह घटना केवल कम प्रतिनिधित्व से कहीं आगे जाती है और इसमें व्यवस्थित अपवर्जन, रूढ़िवादी चित्रण, और प्रभुत्वशाली जाति के दृष्टिकोण को सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित करना शामिल है। [1][2][3][4]
इस अवधारणा में पूर्वाग्रह के कई आयाम शामिल हैं, जिनमें मुख्यतः उच्च जाति के निर्णय निर्माताओं द्वारा संपादकीय द्वारपाल की भूमिका, चुनिंदा समाचार कवरेज जो जाति-आधारित अत्याचारों को कम करके दिखाती है, फ्रेमिंग प्रभाव जो हाशियाकृत समुदायों को कमी के मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और स्रोत चयन जो जाति-संबंधित मुद्दों की चर्चा में उच्च जाति की आवाजों को प्राथमिकता देता है। ये प्रथाएं सामूहिक रूप से उस चीज को बनाती हैं जिसे विद्वान “जातिवादी मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र” कहते हैं जो मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के बजाय उसे मजबूत बनाती है। [2][4][5][6][1]
मीडिया में जातिवादी पूर्वाग्रह के तरीके
जातिवादी पत्रकारिता की अभिव्यक्ति कई आपस में जुड़े तरीकों से काम करती है जिन्हें विद्वानों ने व्यापक शोध के माध्यम से पहचाना है। भाषा और शब्दावली के चुनाव अक्सर जाति पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं, मीडिया संस्थान अक्सर ऐसी कोडेड भाषा का उपयोग करते हैं जो रूढ़िवादिता को मजबूत करती है या ऐसे घुमावदार शब्दों का उपयोग करती है जो जाति-आधारित हिंसा की गंभीरता को कम कर देते हैं। कहानी चयन और प्राथमिकता में स्पष्ट पैटर्न दिखते हैं जहां उच्च जाति समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को दलितों और आदिवासियों की व्यवस्थित समस्याओं की तुलना में असमान कवरेज मिलती है। [1][2][4][7]
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में दृश्य प्रतिनिधित्व लगातार दलित और आदिवासी समुदायों को हाशिये पर रखता है, या तो पूर्ण अनुपस्थिति के माध्यम से या रूढ़िवादी चित्रण के माध्यम से जो मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है। विशेषज्ञ स्रोत पैटर्न उच्च जाति के शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और टिप्पणीकारों के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाते हैं, यहां तक कि जब हाशियाकृत समुदायों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही हो। ये तरीके एक साथ मिलकर एक मीडिया वातावरण बनाते हैं जहां प्रभुत्वशाली जाति के दृष्टिकोण को सामान्य बनाया जाता है जबकि हाशियाकृत आवाजों को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जाता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। [3][4][6][8][9][1]
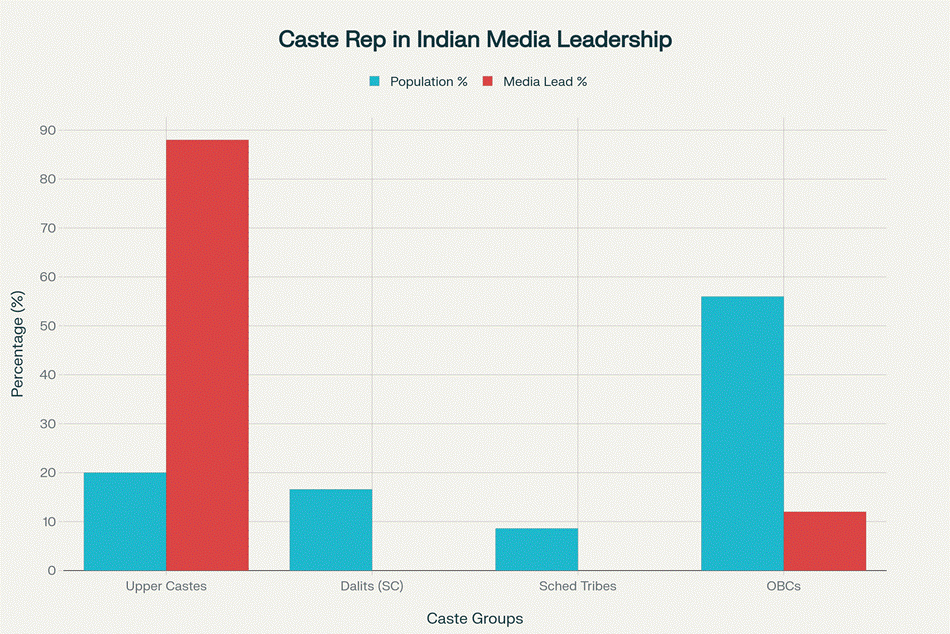
Representation Gap: Population vs Media Leadership in Indian Journalism
व्यवस्थित अपवर्जन के सांख्यिकीय प्रमाण
जातिवादी पत्रकारिता का सबसे ठोस प्रमाण व्यापक मात्रात्मक अध्ययनों से मिलता है जो भारत के मीडिया परिदृश्य में हाशियाकृत समुदायों के चौंकाने वाले कम प्रतिनिधित्व को दस्तावेजित करते हैं। 2019 के ऐतिहासिक ऑक्सफैम-न्यूजलॉन्ड्री अध्ययन, जिसने अंग्रेजी और हिंदी प्रकाशनों में 65,000 से अधिक लेखों का विश्लेषण किया, ने प्रतिनिधित्व में चौंकाने वाली असमानताएं प्रकट कीं। [9][10]
उच्च जातियां, जो भारत की जनसंख्या का केवल 20% हिस्सा हैं, प्रमुख मीडिया संस्थानों में न्यूजरूम नेतृत्व पदों का भारी 88% हिस्सा रखती हैं। यह प्रभुत्व सामग्री निर्माण तक फैला हुआ है, उच्च जाति के पत्रकार अंग्रेजी अखबारों के सभी लेखों का 95% और हिंदी प्रकाशनों का 90% तैयार करते हैं। इसके विपरीत, दलित, जो जनसंख्या का 16.6% हिस्सा हैं, न्यूजरूम नेतृत्व पदों में शून्य प्रतिनिधित्व रखते हैं और अंग्रेजी अखबार लेखों में 5% से भी कम योगदान देते हैं। [10][11][9]
अध्ययन में पाया गया कि प्रमुख बहस शो के हर चार एंकरों में से तीन उच्च जातियों से संबंधित हैं, प्राइम टाइम चर्चा में दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और भी चिंताजनक बात यह है कि प्रमुख बहस शो के 70% से अधिक पैनलिस्ट उच्च जातियों से लिए जाते हैं, जो गूंजने वाले कक्ष बनाते हैं जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर विविध दृष्टिकोणों को बाहर रखते हैं। यह डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत का मीडिया एक विशेष उच्च जाति डोमेन के रूप में कैसे काम करता है जो जनसंख्या के 80% से अधिक की आवाजों को व्यवस्थित रूप से हाशिये पर रखता है। [11][12][9][10]
ऐतिहासिक संदर्भ और विकास
भारत में जातिवादी पत्रकारिता की जड़ें औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिनों में मिलती हैं, जब मीडिया स्वामित्व और संपादकीय नियंत्रण शिक्षित उच्च जाति अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में द हिंदू और द इंडियन मिरर जैसे अखबारों का उदय हुआ, जो अक्सर दलितों और अन्य हाशियाकृत समुदायों को कमी के नजरिए से चित्रित करते थे, औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद को मजबूत करते थे। [1][6][13]
डॉ. बी.आर. अंबेडकर की दूरदर्शी पहचान मीडिया पूर्वाग्रह की ओर 1920 में मूकनायक (मूकों के नेता) की स्थापना की ओर ले गई, जो हाशियाकृत समुदायों के लिए वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। अंबेडकर ने चतुराई से देखा था कि मुख्यधारा मीडिया विशिष्ट जाति हितों की सेवा करता है जबकि दूसरों की चिंताओं के प्रति उदासीन रहता है, मूकनायक के पहले संस्करण में लिखते हुए: “यदि हम बॉम्बे प्रेसीडेंसी में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर केवल एक सरसरी नजर डालें, तो हम पाएंगे कि इन पेपरों में से कई केवल कुछ जातियों के हितों की रक्षा में चिंतित हैं”। [6][13][14]
स्वतंत्रता के बाद की अवधि में इन पूर्वाग्रहों का संस्थागतकरण औपचारिक मीडिया संरचनाओं के माध्यम से हुआ जो उच्च जाति के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते रहे जबकि दलित और आदिवासी आवाजों को हाशिये पर रखते रहे। 1920 से 1940 के दशक दलित पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था, बहिष्कृत भारत और विभिन्न क्षेत्रीय प्रकाशनों के साथ प्रभुत्वशाली कहानियों को चुनौती देते हुए। हालांकि, कॉर्पोरेट नियंत्रण के तहत मुख्यधारा मीडिया के एकीकरण ने धीरे-धीरे इन वैकल्पिक आवाजों को दबा दिया, जिससे प्रतिनिधित्व की वर्तमान संकट की स्थिति आई। [12][13][6]
समकालीन अभिव्यक्तियां और केस स्टडी
आधुनिक जातिवादी पत्रकारिता सूक्ष्म लेकिन व्यापक प्रथाओं के माध्यम से प्रकट होती है जो जाति-संबंधित मुद्दों की सार्वजनिक समझ को आकार देती है। रोहित वेमुला मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे मुख्यधारा मीडिया ने शुरू में युवा विद्वान की आत्महत्या में जाति भेदभाव की भूमिका को कम करके दिखाया, कई आउटलेट्स ने सुझाया कि संस्थागत जातिवाद के अलावा अन्य कारक जिम्मेदार थे। संरचनात्मक जातिवाद से ध्यान हटाने की यह प्रवृत्ति जाति-संबंधित घटनाओं के मीडिया कवरेज में एक सुसंगत पैटर्न है। [1][7][15]
जाति-आधारित हिंसा का कवरेज अक्सर समस्याग्रस्त फ्रेमिंग प्रदर्शित करता है जो कानून व्यवस्था के पहलुओं पर केंद्रित होता है जबकि ऐसी घटनाओं के अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों को नजरअंदाज करता है। राजस्थान के जालोर जिले में अपने शिक्षक द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए नौ साल के दलित लड़के का हालिया मामला इस पैटर्न को दर्शाता है, मुख्यधारा के आउटलेट्स मुख्य रूप से इस पर बहस करते हैं कि घटना “जाति-प्रेरित” थी या नहीं, बजाय उन व्यवस्थित कारकों की जांच के जो ऐसी हिंसा को सक्षम बनाते हैं। [8][16][17][1]
भाषाई पूर्वाग्रह एक और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मीडिया आउटलेट्स अक्सर जाति अत्याचारों का वर्णन करने के लिए घुमावदार भाषा का उपयोग करते हैं जबकि उच्च जाति पीड़ितों के साथ अपराधों के लिए कठोर शब्दावली का उपयोग करते हैं। दृश्य प्रतिनिधित्व पैटर्न लगातार दलित और आदिवासी समुदायों को हाशिये पर रखते हैं, या तो विज्ञापनों और कार्यक्रमों से पूर्ण अनुपस्थिति के माध्यम से या रूढ़िवादी चित्रण के माध्यम से जो मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं। [3][7][18][8]
टेलीविजन प्रोग्रामिंग, विशेष रूप से मनोरंजन मीडिया में, निचली जाति के पात्रों को अशिक्षित, आपराधिक या दासवत के रूप में चित्रित करके हानिकारक रूढ़िवाद को कायम रखती है जबकि सकारात्मक भूमिकाओं में उच्च जाति का प्रभुत्व बनाए रखती है। इन प्रतिनिधित्वों का हाशियाकृत समुदायों के प्रति सार्वजनिक धारणा और सामाजिक दृष्टिकोण पर दूरगामी प्रभाव होता है। [1][3][8]
हाशियाकृत समुदायों और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव
जातिवादी पत्रकारिता के प्रभाव मीडिया प्रतिनिधित्व से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, हाशियाकृत समुदायों के जीवित अनुभवों और व्यापक सामाजिक सामंजस्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। दलित और आदिवासी समुदायों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आंतरिक उत्पीड़न, कम आत्म-सम्मान, और सीमित आकांक्षी क्षितिज शामिल हैं जब उनके समुदायों से सकारात्मक रोल मॉडल और सफलता की कहानियां मुख्यधारा मीडिया में अदृश्य रह जाती हैं। [4][11]
राजनीतिक भागीदारी का नुकसान होता है जब हाशियाकृत समुदायों को मीडिया चर्चा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, सार्वजनिक नीति बहसों और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सामाजिक नीति के बारे में मीडिया चर्चा में विविध आवाजों की अनुपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि हाशियाकृत समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताएं और दृष्टिकोण नीति निर्माण में अनसुलझे रह जाते हैं। [10][12][19]
सामाजिक हिंसा और भेदभाव तब कायम रहते हैं जब मीडिया कवरेज जाति-आधारित अत्याचारों को व्यवस्थित उत्पीड़न के व्यापक पैटर्न के भीतर पर्याप्त रूप से संदर्भित करने में विफल रहती है। जब मीडिया आउटलेट्स जाति हिंसा की अलग घटनाओं को संरचनात्मक भेदभाव के लक्षणों के बजाय विपथन के रूप में मानते हैं, तो वे सार्वजनिक उदासीनता और नीतिगत निष्क्रियता में योगदान देते हैं। [1][7][8][15][17]
आर्थिक प्रभाव तब उभरते हैं जब भेदभावपूर्ण मीडिया प्रथाएं मीडिया उद्योगों में योग्य दलित और आदिवासी पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित करती हैं। यह एक स्व-कायम रखने वाला चक्र बनाता है जहां मीडिया कार्यबल में प्रतिनिधित्व की कमी मीडिया कहानियों और सार्वजनिक चर्चा से अपवर्जन को मजबूत करती है। [11][12][20][4][10]
शैक्षिक प्रभाव तब प्रकट होता है जब हाशियाकृत समुदायों के युवाओं को सकारात्मक मीडिया प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, उनकी करियर आकांक्षाओं और आत्म-धारणा को प्रभावित करता है। मीडिया में सफल दलित और आदिवासी रोल मॉडल्स की अनुपस्थिति इन समुदायों के बीच कम शैक्षिक प्रेरणा और सीमित व्यावसायिक आकांक्षाओं में योगदान देती है। [6][12][14][11]

A woman wearing a pink saree seated indoors, symbolizing the presence and activism of Dalit journalists in Indian media.
वैकल्पिक मीडिया आंदोलन और डिजिटल प्रतिरोध
वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म का उदय मुख्यधारा मीडिया के जातिवादी पूर्वाग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, दलित, बहुजन और आदिवासी समुदाय डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाकर स्वतंत्र कहानी स्थान बना रहे हैं। समकालीन वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे राउंड टेबल इंडिया, दलित कैमरा, द मूकनायक, वेलिवाडा, और जस्टिस न्यूज ने हाशियाकृत आवाजों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। [21][22][23]
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल सक्रियता ने हाशियाकृत समुदायों को अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करने, रूढ़िवाद को चुनौती देने, और भौगोलिक सीमाओं के पार एकजुटता नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाया है। दलित कैमरा यूट्यूब चैनल, उदाहरण के लिए, दलित अनुभवों के अभिलेखागार के रूप में कार्य करता है जबकि समुदायिक संगठन और चेतना जगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। [4][22][23][24]
खबर लहरिया, ग्रामीण उत्तर प्रदेश से सभी महिला मीडिया सामूहिक, इस बात का उदाहरण है कि कैसे हाशियाकृत समुदाय नवीन मीडिया मॉडल बना रहे हैं जो जाति और लिंग दोनों पदानुक्रमों को चुनौती देते हैं। प्रिंट से डिजिटल मीडिया में उनका संक्रमण मीडिया उत्पादन और वितरण के लोकतंत्रीकरण में तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाता है।[11]
हालांकि, इन वैकल्पिक प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें सीमित वित्तीय संसाधन, मुख्यधारा मीडिया की तुलना में प्रतिबंधित पहुंच, तकनीकी बाधाएं, और हाशियाकृत आवाजों को चुप कराने की कोशिश करने वाले प्रभुत्वशाली जाति समूहों द्वारा समन्वित उत्पीड़न अभियान शामिल हैं। डिजिटल विभाजन भी कई दलितों और आदिवासियों के लिए पहुंच को सीमित करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, वैकल्पिक मीडिया पहलों की पहुंच और प्रभाव को बाधित करता है।[10][12][23]

नैतिक निहितार्थ और व्यावसायिक मानक
जातिवादी पत्रकारिता की निरंतरता व्यावसायिक नैतिकता और लोकतांत्रिक समाजों में मीडिया की भूमिका के बारे में मौलिक सवाल उठाती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से रिपोर्टिंग में जाति-आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, यह कहते हुए कि “किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग की पहचान से बचा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब संदर्भ में यह उस जाति के लिए अपमानजनक भावना या गुण या आचरण को व्यक्त करता है”।[25][26][27]
पत्रकारिता सिद्धांतों का उल्लंघन तब होता है जब मीडिया आउटलेट्स जाति-संबंधित मुद्दों का सटीक, निष्पक्ष और व्यापक कवरेज प्रदान करने में विफल रहते हैं। निष्पक्षता का सिद्धांत तब समझौता हो जाता है जब न्यूजरूम में विविध दृष्टिकोणों का अभाव होता है और जब संपादकीय निर्णय समाचार मूल्यों के बजाय जाति पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं।[26][28][25]
पत्रकारिता कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा शायद ही कभी जाति संवेदनशीलता या हाशियाकृत समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करती है। यह शैक्षिक अंतर भविष्य के पत्रकारों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को पहचानने और संबोधित करने के लिए तैयार करने में विफल रहकर अपवर्जन के चक्र को कायम रखता है।[28][29]
जवाबदेही तंत्र कमजोर रहते हैं, प्रेस परिषदों और मीडिया निगरानी संस्थानों के पास जातिवादी रिपोर्टिंग प्रथाओं के खिलाफ सार्थक प्रतिबंध लागू करने का अधिकार या झुकाव का अभाव है। मीडिया नैतिकता प्रवर्तन की स्व-नियामक प्रकृति भेदभावपूर्ण प्रथाओं को न्यूनतम परिणामों के साथ जारी रखने की अनुमति देती है।[27][25][26]
अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता मानक विविधता, समावेश और प्रतिनिधित्व को मुख्य व्यावसायिक मूल्यों के रूप में जोर देते हैं, यह उजागर करते हुए कि भारतीय मीडिया प्रथाएं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से कितनी कम हैं। इन मानकों को लागू करने में विफलता न केवल व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन करती है बल्कि मीडिया विश्वसनीयता और सार्वजनिक भरोसे को भी कमजोर करती है।[29][25][28]

Protesters in India advocate for freedom of expression and press rights, highlighting challenges faced by journalists.
नियामक ढांचा और कानूनी आयाम
भारत का कानूनी और नियामक ढांचा जातिवादी पत्रकारिता को संबोधित करने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है, हालांकि प्रवर्तन समस्याग्रस्त रहता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, और 17 के तहत संवैधानिक प्रावधान जाति-आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, भेदभावपूर्ण मीडिया प्रथाओं को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार बनाते हैं।[25][30]
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सैद्धांतिक रूप से मीडिया सामग्री पर लागू हो सकते हैं जो इन समुदायों के खिलाफ घृणा या भेदभाव को बढ़ावा देती है। हालांकि, मीडिया सामग्री पर इन प्रावधानों का व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रवर्तन चुनौतियों और परिभाषात्मक अस्पष्टताओं के कारण सीमित रहता है।[31][25]
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नियम जाति-संवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए नैतिक दिशानिर्देश स्थापित करते हैं, लेकिन परिषद की अर्ध-न्यायिक शक्तियां दंडात्मक कार्रवाई के बजाय नैतिक निंदा तक सीमित हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्वैच्छिक प्रकृति भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकने में उनकी प्रभावशीलता को कम करती है।[26][27][25]
हाल के कानूनी विकास, जिनमें जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सुकन्या शांता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले शामिल हैं, सार्वजनिक संस्थानों में व्यवस्थित जातिवाद को संबोधित करने की आवश्यकता की बढ़ती न्यायिक मान्यता को दर्शाते हैं। यह मिसाल संभावित रूप से मीडिया संस्थानों तक विस्तारित हो सकती है, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने के लिए नए कानूनी रास्ते बनाती है।[30][32]
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, जिसमें नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD) शामिल है, मीडिया में जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त ढांचे प्रदान करता है। इन अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकने और उपचार करने के दायित्व बनाती हैं।[25]
समाधान और सिफारिशें
जातिवादी पत्रकारिता को संबोधित करने के लिए व्यापक, बहु-हितधारक हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो समस्या के संरचनात्मक, संस्थागत और सांस्कृतिक आयामों को लक्षित करे। विविधता और समावेश पहल को टोकनिस्टिक हायरिंग से आगे जाकर मीडिया संगठनों में सार्थक सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करना चाहिए। इसमें न्यूजरूम, संपादकीय बोर्ड और प्रबंधन पदों में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के लिए न्यूनतम प्रतिनिधित्व लक्ष्य स्थापित करना शामिल है।[9][11][12][14]
पत्रकारिता कार्यक्रमों में शैक्षिक सुधार में जाति संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय रिपोर्टिंग और अंतर-विभागीय विश्लेषण पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। आम जनता के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रम दर्शकों को समाचार सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और रिपोर्टिंग में जाति पूर्वाग्रहों को पहचानने में मदद कर सकते हैं।[18][28][29]
वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वित्तपोषण तंत्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नागरिक समाज समर्थन और नवीन वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से मजबूत बनाने की आवश्यकता है जो जाति-विशेषाधिकार प्राप्त व्यापारों से विज्ञापन राजस्व पर निर्भरता को कम करे। प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हाशियाकृत आवाजों के उत्पीड़न और दमन को रोकने और विविध सामग्री को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू कर सकते हैं।[12][14][19][21][18]
नियामक सुदृढ़ीकरण में भेदभावपूर्ण प्रथाओं की जांच और दंड के लिए प्रेस परिषदों की बढ़ी हुई शक्तियां शामिल होनी चाहिए, साथ ही जाति-संवेदनशील रिपोर्टिंग पर स्पष्ट दिशानिर्देश भी। व्यावसायिक संघों के माध्यम से उद्योग स्व-नियमन समावेशी पत्रकारिता प्रथाओं पर केंद्रित सहकर्मी समीक्षा तंत्र और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम स्थापित कर सकता है।[25][26][27][28][29]
समुदाय-आधारित निगरानी पहल जातिवादी पत्रकारिता के उदाहरणों का दस्तावेजीकरण कर सकती हैं और हाशियाकृत समुदायों के बेहतर कवरेज की वकालत कर सकती हैं। मुख्यधारा और वैकल्पिक मीडिया के बीच सहयोग मुख्यधारा कहानियों में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए मार्ग बना सकता है जबकि वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म में क्षमता निर्माण कर सकता है।[7][14][17][21][22][18]
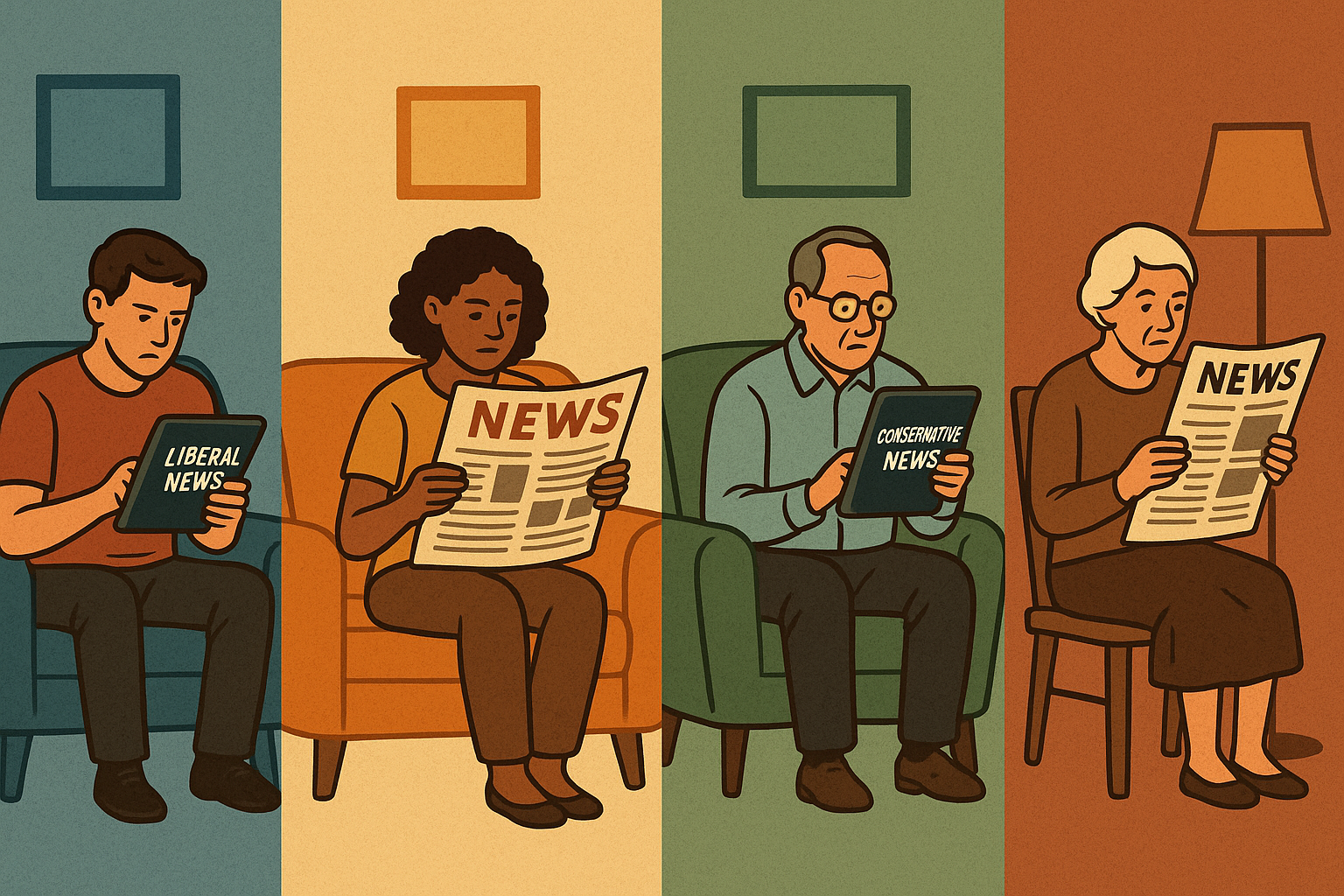
वैश्विक संदर्भ और तुलनात्मक दृष्टिकोण
भारत में जातिवादी पत्रकारिता की चुनौती नस्ल, जातीयता और सामाजिक वर्ग के आधार पर मीडिया भेदभाव के व्यापक वैश्विक पैटर्न के साथ प्रतिध्वनित होती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दिखाता है कि दुनिया भर में हाशियाकृत समुदाय मुख्यधारा मीडिया में अपवर्जन, गलत प्रतिनिधित्व और रूढ़िवाद के समान पैटर्न का सामना कैसे करते हैं[33]

Global overview of research on digital media’s impacts on democracy, content features, and political outcomes across countries and methods.
। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य लोकतांत्रिक समाजों के अध्ययन समानांतर संरचनात्मक पूर्वाग्रह प्रकट करते हैं जो प्रभुत्वशाली समूहों को विशेषाधिकार देते हैं जबकि अल्पसंख्यकों को हाशिये पर रखते हैं।
डिजिटल मीडिया का दोहरा प्रभाव वैश्विक रुझानों को दर्शाता है जहां तकनीक एक साथ सामग्री निर्माण का लोकतंत्रीकरण करती है जबकि मौजूदा शक्ति संरचनाओं को दोहराती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय ने वैश्विक स्तर पर हाशियाकृत आवाजों के लिए नए अवसर बनाए हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म समन्वित उत्पीड़न अभियानों और भेदभावपूर्ण सामग्री के प्रसार को भी सक्षम बनाते हैं।[18][19]
अन्य देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं में मीडिया संगठनों में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां, विविध मीडिया सामग्री के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण, और नियामक ढांचे शामिल हैं जो केवल भेदभाव को प्रतिबंधित करने के बजाय सक्रिय रूप से समावेश को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न देशों में मीडिया विकास कार्यक्रम दिखाते हैं कि कैसे लक्षित हस्तक्षेप विविधता बढ़ा सकते हैं और हाशियाकृत समुदायों का कवरेज सुधार सकते हैं।[28][29]
मानवाधिकार संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकालत प्रयास तेजी से मीडिया प्रतिनिधित्व को व्यापक समानता और न्याय पहलों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने मीडिया विविधता का आकलन करने और समावेशी पत्रकारिता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ढांचे विकसित किए हैं जो भारतीय नीति हस्तक्षेपों को सूचित कर सकते हैं।[25]
तकनीकी परिवर्तन और भविष्य की संभावनाएं
भारत के मीडिया परिदृश्य का तेजी से डिजिटलीकरण जातिवादी पत्रकारिता को संबोधित करने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। सामग्री वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदमिक निर्णय लेना या तो मौजूदा पूर्वाग्रहों को बढ़ा सकता है या विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स प्रतिनिधित्व पैटर्न को ट्रैक करने और समावेश लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को मापने में मदद कर सकता है।[9][10][19]
पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग सेवाओं और स्वतंत्र डिजिटल चैनलों जैसे उभरते प्लेटफॉर्म हाशियाकृत आवाजों के लिए नई जगहें बना रहे हैं, हालांकि पहुंच आर्थिक और तकनीकी बाधाओं द्वारा सीमित रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल तकनीक की पैठ पहले से बाहर रखे गए दर्शकों तक वैकल्पिक कहानियों के साथ पहुंचने के अवसर प्रदान करती है।[11][21][23][24]
मीडिया उपभोक्ताओं के बीच पीढ़ीगत परिवर्तन, विशेष रूप से युवा दर्शक जो विविध दृष्टिकोणों और सामाजिक न्याय सामग्री के लिए अधिक ग्रहणशील हैं, समावेशी पत्रकारिता के लिए बाजार प्रोत्साहन बनाता है। क्राउडफंडिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स को पारंपरिक विज्ञापन और कॉर्पोरेट प्रायोजन पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाते हैं।[14][21][29]
वर्चुअल और संवर्धित वास्तविकता तकनीकें immersive कहानी कहने की नई संभावनाएं प्रदान करती हैं जो रूढ़िवाद को चुनौती दे सकती हैं और जाति रेखाओं के पार सहानुभूति निर्माण कर सकती हैं। ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत तकनीकें संभावित रूप से हाशियाकृत आवाजों के लिए सेंसरशिप-प्रतिरोधी प्लेटफॉर्म बना सकती हैं।[19][23]
निष्कर्ष
जातिवादी पत्रकारिता भारत के लोकतांत्रिक मीडिया परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है, जो संरचनात्मक असमानताओं को बनाए रखती है जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को कमजोर करती है। मुख्यधारा मीडिया से हाशियाकृत आवाजों का व्यवस्थित अपवर्जन न केवल व्यावसायिक पत्रकारिता नैतिकता का उल्लंघन करता है बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के लिए भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता में भी बाधा डालता है।
प्रस्तुत साक्ष्य दिखाते हैं कि मीडिया स्वामित्व, संपादकीय नियंत्रण और कहानी निर्माण के वर्तमान पैटर्न जाति पदानुक्रम को चुनौती देने के बजाय उन्हें मजबूत बनाने का काम करते हैं। यह स्थिति तत्काल, व्यापक हस्तक्षेप की मांग करती है जो भारत के मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर भेदभाव के संरचनात्मक, संस्थागत और सांस्कृतिक आयामों को संबोधित करे।
वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रतिरोध आंदोलनों का उदय परिवर्तनकारी परिवर्तन की आशा प्रदान करता है, लेकिन इन पहलों को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए निरंतर समर्थन और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है। आगे का रास्ता वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि मीडिया परिदृश्य बनाने के लिए मीडिया संगठनों, नागरिक समाज, सरकारी संस्थानों और स्वयं हाशियाकृत समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।
केवल इस तरह के व्यापक परिवर्तन के माध्यम से भारत का मीडिया सभी आवाजों और दृष्टिकोणों के लिए एक मंच के रूप में सेवा करने के अपने लोकतांत्रिक जनादेश को पूरा कर सकता है, अधिक न्यायसंगत और समान समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। निहितार्थ मीडिया प्रतिनिधित्व से कहीं आगे तक फैले हुए हैं और समकालीन भारत में लोकतंत्र, नागरिकता और सामाजिक सामंजस्य के व्यापक प्रश्नों को समेटते हैं।
कॉस्मेटिक बदलाव और टोकन इशारों का समय बीत चुका है; अब जिस चीज की आवश्यकता है वह मौलिक संरचनात्मक सुधार है जो मीडिया विविधता और समावेश को धर्मार्थ दायित्वों के रूप में नहीं बल्कि एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों के रूप में पहचानता है। भारतीय पत्रकारिता—और वास्तव में भारतीय लोकतंत्र—का भविष्य मीडिया की जाति-आधारित अपवर्जनों को पार करने और अपनी सामाजिक उत्पत्ति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की सेवा करने वाली वास्तव में सार्वजनिक संस्था के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करता है।
- https://journal.hmjournals.com/index.php/JMCC/article/download/1708/2003/3324
- https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/2019-08/Oxfam NewsLaundry Report_For Media use.pdf
- https://www.ijraset.com/research-paper/caste-gender-and-media-stereotypes
- https://www.polecom.org/index.php/polecom/article/download/162/406/770
- https://www.apc.org/en/news/proposal-caste-ing-out-media-exploring-role-media-plays-ushering-caste-sensitive-society
- https://feminisminindia.com/2020/04/03/rise-fall-dalit-journalism-india/
- http://onlineregistration.bgco.ca/news/subtle-caste-bias-in-media
- https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5038699.pdf?abstractid=5038699&mirid=1
- https://idsn.org/report-dalits-and-adivasis-missing-from-mainstream-indian-news-media-dominant-castes-dominate-leadership-positions/
- https://sprf.in/wp-content/uploads/2024/12/SPRF-2021_Dalit-Media_Final.pdf
- https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/04/04/980097004/indias-lowest-caste-has-its-own-news-outlet-and-shes-in-charge
- https://www.dw.com/en/india-dalit-journalists-give-a-voice-to-the-marginalized/a-66067288
- https://www.nytimes.com/2023/03/06/world/asia/india-caste-discrimination-dalit-journalist-mooknayak.html
- https://nextcity.org/urbanist-news/journalists-from-indias-lowered-castes-are-making-their-stories-known
- https://www.pbs.org/newshour/world/how-one-woman-defies-caste-discrimination-in-india
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5038699
- https://www.fairplanet.org/story/in-their-own-words-dalit-journalists-challenge-media-bias/
- https://www.theswaddle.com/by-stifling-marginalized-voices-social-media-mimics-real-life-casteism
- https://www.ijirct.org/download.php?a_pid=2406074
- https://www.statecraft.co.in/article/dalit-journalists-indian-mainstream-media-a-manifestation-of-caste-and-class-privilege
- https://www.hindustantimes.com/india-news/meet-the-dalits-who-are-using-online-platforms-to-tell-stories-of-their-community/story-nkg4lHQ1DL44DbCBiJ7CrN.html
- https://www.roundtableindia.co.in/dalits-and-social-media/
- https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue2/Version-5/R01925125129.pdf
- https://jmi.ac.in/upload/advertisement/ccmg_PrePhD_2023september18.pdf
- https://www.tezu.ernet.in/tu_codl/slm/Open/MAMCD/2/MMC-201-BLOCK-II.pdf
- https://www.presscouncil.nic.in/WriteReadData/PDF/Norms2010.pdf
- http://www.mahratta.org/CurrIssue/2019_March/March19_4.pdf
- https://thekashmirhorizon.com/2024/03/19/role-of-ethics-and-law-in-indian-journalism/
- https://aaft.edu.in/blog/what-are-the-ethics-of-journalism-in-india
- https://blog-iacl-aidc.org/2024-posts/2024/12/5/the-case-of-caste-based-discrimination-in-indian-prisons-a-new-constitutional-right-to-overcome-prejudice
- https://desikaanoon.in/media-coverage-on-sensitive-issues-an-analysis-on-law-and-ethics-of-media-reporting/
- https://m.thewire.in/article/caste/full-text-why-a-journalist-filed-a-petition-against-caste-based-practices-in-indias-prisons
- http://archives.christuniversity.in/disk0/00/00/71/89/01/1424054_Tessy_Jacob_28_Nov_PM.pdf