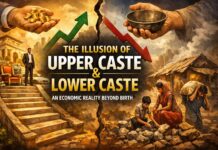हिन्दू विधि के अंतर्गत विभाजन: मिताक्षरा स्कूल का व्यापक विश्लेषण
हिन्दू विधि में विभाजन संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व से व्यक्तिगत स्वामित्व में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मिताक्षरा स्कूल, जो भारत के अधिकांश भाग में लागू है, विभाजन की प्रक्रिया में दायभाग पद्धति से मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
मिताक्षरा विधि के अनुसार विभाजन का अर्थ
विभाजन के द्वैत अर्थ
मिताक्षरा विधि में विभाजन के दो भेद स्पष्ट किए गए हैं:
- “समूची पारिवारिक संपत्ति के अधिकारों को निश्चित भागों में विभाजित करना”
- “संयुक्त स्थिति का वह विच्छेद, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी प्रभाव उत्पन्न होते हैं”
विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें सहदायिकता के परिवर्ती हित को एक निश्चित हिस्से में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सह-स्वामी को पूरी संपत्ति का सह-स्वामी माना जाता है, परंतु विभाजन के पश्चात उनकी स्वामित्व सीमित भाग में ही रह जाती है—इसी को “पूरी संपत्ति में स्वामित्व का सिद्धांत” कहते हैं।
विभाजन का सारः स्थिति का विच्छेद
मिताक्षरा विभाजन का मुख्य सार है “संयुक्त स्थिति का विच्छेद”; शारीरिक विभाजन आवश्यक नहीं, बल्कि पारिवारिक सदस्य का “अलग होने का इरादा” ही विभाजन को पूर्ण करता है। जब सदस्य यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि वह सहदायिक नहीं रहना चाहता, तभी कानूनी विभाजन संपन्न हो जाता है।
अधिकारों का विभाजन एवं संपत्ति का विभाजन
विभाजन दो चरणों में होता है:
- अधिकारों का विभाजन: प्रत्येक सहदायिक के हिस्से को इरादे सहित निश्चित करना
- संपत्ति का विभाजन: वास्तविक संपत्ति को उन हिस्सों के अनुसार आवंटित करना
पहला चरण कानूनी रूप से विभाजन पूर्ण करता है; दूसरा चरण उसका कार्यान्वयन है।
विभाजन के लिए योग्य संपत्ति
- केवल सहदायिक संपत्ति विभाजन के लिए योग्य है; व्यक्तिगत संपत्ति विभाजन के अधीन नहीं होती।
- विभाजनात्मक स्थिति के बाद अर्जित संपत्ति अथवा व्यक्तिगत निधियों से खरीदी गई संपत्ति विभाजन से बाहर मानी जाती है।
- कुछ संपत्तियाँ विभाज्य नहींं होतीं, जैसे:
- अविभाज्य संपत्ति: स्वतंत्र रूप से एक सदस्य को मिलने वाली
- प्रकृति से अविभाज्य: पशु, फर्नीचर आदि
- पारिवारिक मूर्तियाँ एवं पूजा स्थल
- वह व्यक्तिगत संपत्ति जो साझा अधिकार के बाहर है
विभाजन से पूर्व निम्न व्यय पहले अलग किए जाते हैं:
- संयुक्त परिवार के कर्ज
- पिता के व्यक्तिगत देय दायित्व
- आश्रित महिला सदस्यों का भरण-पोषण
- अविवाहित कन्याओं का विवाह व्यय
- विधवा माता एवं पारिवारिक अंत्येष्टि व्यय
विभाजन की माँग करने वाले पक्ष
- पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र: पूर्ण पुरुष सहदायिक, पिता की सहमति विना विभाजन माँग सकते हैं, परंतु पिता अपनी पिता/भाईयों सहित पहले से पृथक न हों तो पिता की सहमति आवश्यक।
- गर्भ में संतान: माता के गर्भ में विभाजन समय उपस्थित पुत्र अपना हिस्सा माँग सकता है; बाद में जन्मा पुत्र केवल पिता के आरक्षित हिस्से का वारिस होता है, विभाजन पुनः नहीं खोल सकता।
- बाह्य सम्बन्धी पुत्र: विधिवत् मान्यता प्राप्त परंतु पुत्रत्व रहित वर्ग के अवैध पुत्र को विभाजन नहीं, परन्तु भरण-पोषण का अधिकार।
- विधवा: हिन्दू महिला संपत्ति अधिनियम, 1937 व उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विभाजन का दावा कर सकती है; आवासीय अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
- हस्तांतर प्राप्तकर्ता (Alienee): वैध विभादान से सहदायिक का हिस्सा क्रेत् تقسیم का हकदार होता है।
- विवाहिता पुत्रियाँ (2005 संशोधन के बाद): अब जन्म से सहदायिक; विभाजन और बराबर हिस्से के अधिकारी।
- गोद लिए पुत्र: प्राकृतिक पुत्र की भाँति विभाजन माँग सकते हैं।
विभाजन के तरीके
- घोषणा द्वारा विभाजन: विद्वेषरहित मनोवृत्ति प्रदर्शित करना पर्याप्त।
- नोटिस द्वारा विभाजन: अन्य सहदायिकों को लिखित सूचना देकर।
- वसीयत द्वारा विभाजन: स्पष्ट इच्छापत्र के माध्यम से।
- धर्म परिवर्तन: अन्य धर्म ग्रहण करते ही संयुक्त स्थिति स्वतः विच्छेदित।
- विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह: विवाह से स्थिति विच्छेदित।
- समझौता द्वारा विभाजन: परस्पर लिखित समझौता।
- मध्यस्थता द्वारा विभाजन: मध्यस्थ का निर्णय विभाजन समान प्रभावी।
- पित्र अधिकार द्वारा विभाजन: पिता के एकतरफा आदेश से।
- मुकदमे द्वारा विभाजन: विभाजन मुकदमा दायर करते ही संयुक्त स्थिति समाप्त।
ये तरीके निरपेक्ष नहीं; किसी भी परिस्थिति में यदि “अलग होने की स्पष्ट मंशा” सिद्ध हो जाए, विभाजन मान्य होगा।
विभाजन पुनः खोलने के प्रश्न
अविच्छेद्यता का मूल नियम
मनु के अनुसार:
“विभाजन एक बार हो, विवाह एक बार हो, दान एक बार हो—ये सदैव अपरिवर्तनीय होते हैं।”
पुनः उद्घाटन के अपवाद
- गर्भ में संतान: विभाजन समय गर्भ में पुत्र हिस्सा न मिलने पर पुनः खोल सकता है।
- नाबालिग सहदायिक: अल्पावधि विभाजन असमान होने पर, परिपक्व होते ही पुनः खोल सकता है।
- विधवा द्वारा गोद ली संतान: गोद लेने पर पुनः खोलने का हक।
- अनियमित लाभ: जब कोई सदस्यों ने छल, दबाव या धूर्तता से हानि पहुँचाई हो।
- नदारद सहदायिक: जिन्होंने विभाजन में हिस्सा न पाया हो, लौटने पर पुनः खोल सकते हैं।
- अवशिष्ट संपत्ति: विभाजन में छूटी संपत्ति मिलने पर।
न्यायालयिक दिशानिर्देश
- संयुक्त इरादे से किया गया विभाजन केवल ठगी, दबाव या मिथ्या प्रस्तुति पर ही खोला जा सकता है।
- नाबालिग हितों के लिए विभाजन कभी भी पुनः खोला जा सकता है, समय सीमा रहित।
आधुनिक कानूनी परिवेश
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005
- लिंग समानता: पुत्रियों को जन्म से बराबरी का अधिकार।
- पूर्वव्यापी प्रभाव: 2005 से पहले जन्मी कन्याएँ भी लाभान्वित।
- धारा 23 का उन्मूलन: आवासीय संपत्ति विभाजन अपवाद समाप्त।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
- विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा: पुत्रियों के अधिकार पिता के जीवित होने की स्थिति से स्वतंत्र। lawfinderlive
निष्कर्ष
मिताक्षरा विधि के तहत विभाजन का मूल “स्थिति का विच्छेद” है, जिसमें सहदायिकता के अधिकार को एक निश्चित हिस्से में बदलकर व्यक्तिवादी स्वामित्व सुनिश्चित किया जाता है। विभाजन के अनेक तरीके और पुनः उद्घाटन के सुस्पष्ट अपवाद इसे पारिवारिक और सामाजिेक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक लचीला तंत्र बनाते हैं। 2005 के संशोधन ने इसमें लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के नए आयाम जोड़े हैं, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवार की संस्थात्मक संरचना का समतामूलक रूप से संवर्धन हुआ है।