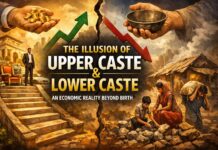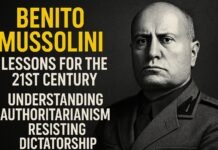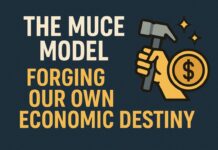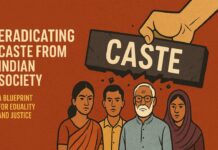ग्रामीण उत्पीड़न से मुक्ति: कैसे शहर सहकारी नेटवर्क के माध्यम से शरण और सशक्तिकरण प्रदान करते हैं
ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकता हाशिए के समुदायों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा, भेदभाव और अमानवीयकरण का एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है जो उन्हें बुनियादी मानवीय गरिमा की तलाश में अपने पैतृक गांवों से भागने के लिए मजबूर करता है। जातिगत हिंसा से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक, बुनियादी सेवाओं से वंचना से लेकर जीवन-घातक उत्पीड़न तक – अपने गांवों में अमानवीय व्यवहार का सामना कर रहे उत्पीड़ित और दलित समुदायों के लिए शहरी प्रवासन केवल एक आर्थिक अवसर नहीं बल्कि अस्तित्व और गरिमा की दिशा में एक हताश उड़ान का प्रतिनिधित्व करता है। समान समुदाय निवास करने वाले शहरों में रणनीतिक बसावट, मजबूत सहकारी नेटवर्क के विकास के साथ मिलकर, इन कमजोर आबादियों को ग्रामीण उत्पीड़न से शहरी सशक्तिकरण तक का रास्ता प्रदान करती है।
हाल के दस्तावेजों से हाशिए के समुदायों के खिलाफ ग्रामीण हिंसा के चिंताजनक पैमाने का पता चलता है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के 60,000 से अधिक मामले सालाना दर्ज किए जाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश मामले अनदर्ज रह जाते हैं। क्रूरता अक्सर अपनी आकस्मिक निर्दयता में चौंकाने वाली होती है: एक नौ साल के दलित लड़के को “उच्च जाति” के बर्तन से पानी पीने के लिए पीट-पीटकर मार डाला जाना, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग न लेने के लिए दलित परिवारों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार, गांव के कुओं से पानी इकट्ठा करने की कोशिश करने पर महिलाओं पर हमला, और जाति पदानुक्रम के छोटे से छोटे कथित उल्लंघन के लिए निरंतर हिंसा के खतरे में जी रही पूरी आबादी।
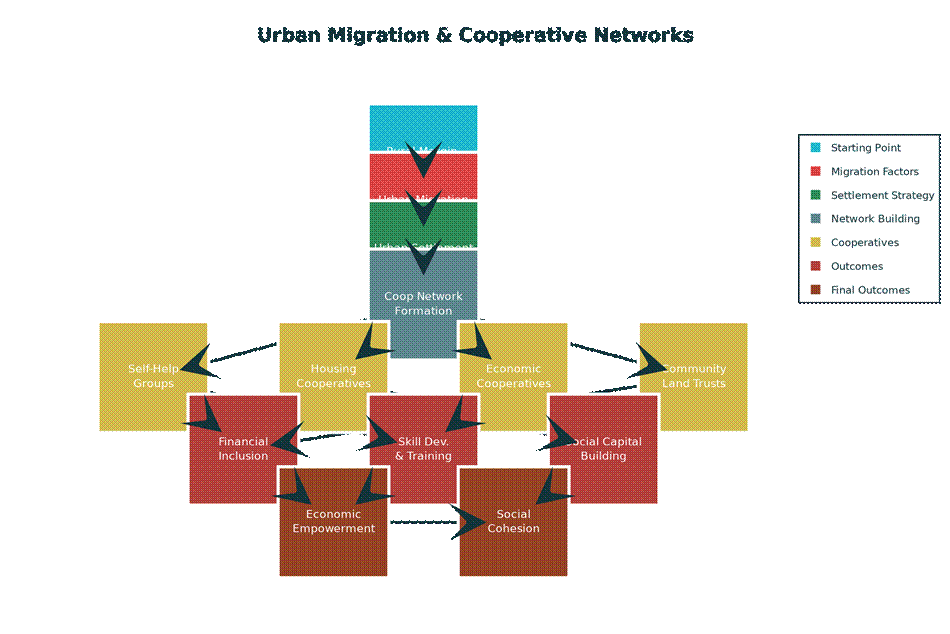
Urban Migration and Cooperative Network Development Pathway for Marginalized Communities
ग्रामीण उत्पीड़न की क्रूर वास्तविकता
व्यवस्थित हिंसा और अमानवीयकरण
ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए के समुदायों पर की जाने वाली हिंसा अलग-थलग घटनाओं से कहीं अधिक है—यह कठोर सामाजिक पदानुक्रमों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए अमानवीयकरण के एक व्यवस्थित पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के गांवों में, दलितों और अन्य हाशिए के समूहों को ऐसी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है जो किसी भी सभ्य समाज में अकल्पनीय होंगी: गांव के कुओं का उपयोग करने से मना, मंदिरों में प्रवेश से रोक, उच्च जातियों के समान स्तर पर बैठने पर रोक, या यहां तक कि उच्च जाति के व्यक्तियों पर अपनी छाया डालने से भी मनाही।
हरिजन सेवक संघ के 1,155 गांवों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 613 गांवों में अछूतों को गांव के कुओं तक पहुंच से वंचित किया गया और 821 गांवों में मंदिरों से रोका गया। इन प्रतिबंधों को इतनी गंभीर हिंसा के माध्यम से लागू किया जाता है कि यह समझ से परे है: दलितों को मल खाने पर मजबूर करना, उन्हें नग्न होकर सड़कों पर परेड कराना, उनके घरों को जलाना, और जाति प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन की सजा के रूप में यौन हमले करना।
कर्नाटक के 2015 के मरुकुंबी गांव का मामला ग्रामीण उत्पीड़न की समन्वित प्रकृति का उदाहरण देता है। जब दलितों को स्थानीय नाई की दुकानों और होटलों में प्रवेश से मना कर दिया गया, तो 117 लोगों ने दलित झोपड़ियों में आग लगाने और निवासियों पर हमला करने की साजिश रची। इस मामले के परिणामस्वरूप 101 दोषसिद्धि हुईं—माना जाता है कि यह पहला मामला था जहां अस्पृश्यता संबंधी मामले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दोषी पाया गया। दुखद बात यह है कि वीरेश मरकुंबी, एक प्रमुख गवाह और इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता, को उसी सुबह रेलवे पटरी पर मृत पाया गया जब उसे अदालत में गवाही देनी थी।
आर्थिक बंधन और सामाजिक बहिष्करण
शारीरिक हिंसा से परे, ग्रामीण हाशिए के समुदायों को व्यवस्थित आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है जो उनकी भेद्यता को कायम रखता है। गांधी शांति फाउंडेशन के सर्वेक्षण में 10 राज्यों में 2.6 मिलियन बंधुआ मजदूर मिले, जिनमें से 62% अछूत और अन्य 25% आदिवासी समुदायों से थे। ये परिवार दिन में केवल 15-35 रुपये (US$0.38-0.88) या कुछ किलो चावल के लिए काम करते हैं, कर्ज की बंधन के चक्र में फंसे हुए जो पीढ़ियों तक चलता है।
सर्वेक्षण से पता चला कि विधायकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के रिश्तेदार और समर्थक बंधुआ मजदूरी कराने वालों में शामिल थे, जो शोषण की संस्थागत प्रकृति को उजागर करता है। पुलिस अधिकारी खुले तौर पर अस्पृश्यता विरोधी कानूनों को लागू करने की अपनी अनिच्छा स्वीकार करते हैं, एक तमिलनाडु अधिकारी के इन शब्दों के साथ: “अगर हम इस कानून को गंभीरता से लें, तो तमिलनाडु की आधी आबादी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। वैसे भी, पुलिस के पास लोगों के निजी मामलों में नाक घुसाने से बेहतर काम हैं”।
राज्य की मिलीभगत और न्यायिक विफलताएं
शायद सबसे निराशाजनक बात हाशिए के समुदायों की सुरक्षा के लिए राज्य संस्थानों की व्यवस्थित विफलता है। दलितों के खिलाफ अपराधों के 96% मामले और आदिवासियों के खिलाफ 95% मामले अभी भी मुकदमे की प्रतीक्षा में हैं, जिससे दंडमुक्ति का माहौल बनता है जो अपराधियों का हौसला बढ़ाता है। कई मामलों में, पुलिस अधिकारी खुद जातिगत हिंसा में भाग लेते हैं या हाशिए के पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने से इनकार करते हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट करता है कि एक साल में पुलिस के खिलाफ 68,160 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें हत्या और यातना से लेकर शिकायतें दर्ज करने से इनकार तक की गतिविधियां शामिल थीं। इनमें से 62% को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया, और केवल 26 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। यह संस्थागत विफलता हाशिए के समुदायों के लिए अपने गांवों से भागने के अलावा कोई सहारा नहीं छोड़ती।
मुक्ति और गुमनामी के स्थान के रूप में शहर
डॉ. अम्बेडकर का शहरी शरणस्थली का दृष्टिकोण
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, भारत के संविधान के शिल्पकार और दलित अधिकारों के चैंपियन, ने पहचाना था कि शहर गुमनामी और उन कठोर जाति पदानुक्रमों से बचने के अवसर प्रदान करते हैं जो ग्रामीण जीवन को परिभाषित करते हैं। उनका दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित था कि शहरी स्थान पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को कमजोर कर सकते हैं और हाशिए के व्यक्तियों को जन्म के बजाय क्षमता के आधार पर नई पहचान बनाने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
अम्बेडकर की गांवों की प्रसिद्ध आलोचना “स्थानीयता के गंदे नाले, अज्ञानता के अड्डे, संकीर्णता के केंद्र” के रूप में उनकी इस गहरी समझ को दर्शाती थी कि ग्रामीण स्थान संरचनात्मक रूप से उत्पीड़न को कायम रखने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। उन्होंने शहरीकरण को जाति-प्रभुत्व वाले ग्रामीण जीवन से उन स्थानों की ओर एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जहां जाति वंशावली के बजाय आर्थिक सफलता सामाजिक स्थिति निर्धारित कर सकती है।
समकालीन शोध अम्बेडकर के दृष्टिकोण के पहलुओं की पुष्टि करता है। शहरी वातावरण वास्तव में अधिक गुमनामी और पारंपरिक जाति चिह्नकों की कम दृश्यता प्रदान करता है। दिल्ली आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी जीवनशैली और पोशाक जाति या धार्मिक अंतर को दृश्य संकेतकों के माध्यम से पहचानना विशेष रूप से कठिन बनाते हैं। यह गुमनामी हाशिए के व्यक्तियों को उन दैनिक अपमानों और प्रतिबंधों से बचने की अनुमति देती है जो ग्रामीण जाति पदानुक्रम को परिभाषित करते हैं।
शहरी गुमनामी और पहचान पुनर्निर्माण
हाशिए के प्रवासियों के लिए, शहर ऐसे स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पारंपरिक पहचानों को चुनौती दी जा सकती है और पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि एक अध्ययन प्रतिभागी ने कहा: “दिल्ली में, कोई भी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता कि आप क्या हैं, यहां सभी बाहरी हैं, यहां-वहां से आए हैं, सभी मिलकर रहते हैं”। यह मिश्रण वह पैदा करता है जिसे विद्वान “कॉस्मोपॉलिटन पड़ोसीपन” कहते हैं—एक ऐसी स्थिति जहां विविध समुदायों को सामाजिक सामंजस्य बनाए रखते हुए मतभेदों पर बातचीत करनी पड़ती है।
शहरी अनुभव प्रवासियों को आवश्यक आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हुए गांव-आधारित उत्पीड़न से खुद को दूर करने की अनुमति देता है। गांव प्रतीकात्मक रूप से “सती और अस्पृश्यता” और “जाति, नृजातीय और धार्मिक अलगाव” से जुड़े होते हैं, जबकि शहर “स्वयं को गुमनाम बनाने और अंतर के सबसे हिंसक और दमनकारी रूपों को चुनौती देने की संभावनाएं” प्रदान करते हैं।
हालांकि, यह परिवर्तन न तो पूर्ण है और न ही समस्यारहित। शहरी गुमनामी भेदभाव और बहिष्करण के नए रूपों के साथ सह-अस्तित्व रखती है। जबकि शहर कुछ प्रकार की जातिगत हिंसा को कम कर सकते हैं, वे अक्सर आवासीय पृथक्करण, रोजगार भेदभाव, और सामाजिक बहिष्करण के नए पैटर्न बनाते हैं।
रणनीतिक बसावट: समुदाय और स्थान का चुनाव
शहरी क्षेत्रों में सामाजिक नेटवर्क का महत्व
शोध लगातार प्रदर्शित करता है कि सफल शहरी प्रवासन समान सामुदायिक पृष्ठभूमि के मौजूदा सामाजिक नेटवर्क की उपस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब हाशिए के व्यक्ति शहरों में जाते हैं, तो वे आम तौर पर उन क्षेत्रों में बसते हैं जहां उनकी अपनी जाति या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के लोग पहले से स्थापित हैं। यह समूहीकरण केवल आराम की बात नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीवित रहने की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो आवश्यक सामाजिक पूंजी, आर्थिक अवसर और शहरी भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रमुख भारतीय शहरों के अध्ययन दिखाते हैं कि जाति के आधार पर आवासीय पृथक्करण अक्सर शहरी क्षेत्रों में बना रहता है या तेज़ हो जाता है। जबकि यह शुरू में समस्याजनक लग सकता है, यह वास्तव में केंद्रित समुदाय बनाता है जो पारस्परिक समर्थन और आर्थिक उन्नति के लिए सामूहिक रूप से संगठित हो सकते हैं। ये बस्तियां “शहरी गांवों” के रूप में काम करती हैं जो ग्रामीण मूल और शहरी आकांक्षाओं के बीच पुल का काम करते हैं।
समान समुदायों की एकाग्रता ऐसे नेटवर्क बनाती है जो प्रदान करते हैं:
- प्रारंभिक आवास और शहरी जीवन का अभिविन्यास
- विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर नौकरी रेफरल और रोजगार के अवसर
- अनौपचारिक ऋण नेटवर्क के माध्यम से साख और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच
- आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक संकट के दौरान सामाजिक समर्थन
- विदेशी शहरी वातावरण में सांस्कृतिक निरंतरता और पहचान संरक्षण
- शहरी अधिकारियों या नियोक्ताओं के साथ व्यवहार करते समय सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति
भौगोलिक निकटता और क्षेत्रीय लाभ
शहरी प्रवासन पर विचार कर रहे हाशिए के समुदायों के लिए, अपने गृह राज्य के भीतर निकटवर्ती शहरी केंद्रों का रणनीतिक चयन लंबी दूरी के अंतर्राज्यीय आंदोलन की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण समुदायों को राज्य-विशिष्ट आरक्षण लाभ, शैक्षणिक अवसर और लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बनाए रखने की अनुमति देता है जबकि शहरी आर्थिक अवसरों तक पहुंचता है।
दिल्ली आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश झुग्गी निवासी पड़ोसी राज्यों से आते हैं: उत्तर प्रदेश (48.7%), राजस्थान (17.5%), और बिहार (15%)। इन प्रवासियों में से 53% अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं, 21% अन्य पिछड़े वर्गों से, और 12% मुस्लिम के रूप में पहचान करते हैं। यह भौगोलिक एकाग्रता प्रवासियों को भाषाई परिचितता, सांस्कृतिक संबंध, और मौजूदा सामाजिक नेटवर्क तक पहुंच बनाए रखने की अनुमति देती है जबकि नई शहरी पहचान बनाते हैं।
निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों की प्राथमिकता चक्रीय प्रवासन पैटर्न की सुविधा भी देती है जो परिवारों को शहरी क्षमताओं का निर्माण करते समय ग्रामीण संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। यह ग्रामीण से शहरी आजीविका के क्रमिक संक्रमण को सक्षम बनाते हुए प्रवासन जोखिमों को कम करता है।
जीवित रहने और सशक्तिकरण के लिए सहकारी नेटवर्क का निर्माण
स्वयं सहायता समूह: शहरी एकीकरण की नींव
स्वयं सहायता समूह हाशिए के शहरी प्रवासियों के लिए सहकारी संगठन का सबसे सुलभ और तुरंत लाभकारी रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। 15-25 सदस्यों के ये छोटे संघ महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करते हैं जो औपचारिक बैंकिंग सिस्टम अक्सर नए शहरी प्रवासियों से इनकार करते हैं। ग्रामीण उत्पीड़न से भाग रहे समुदायों के लिए, SHGs क्रेडिट, बचत सुविधाओं और आर्थिक योजना संसाधनों तक पहली सुरक्षित पहुंच प्रदान करते हैं।
शहरी SHGs की सफलता सामाजिक पूंजी निर्माण के साथ वित्तीय सेवाओं के संयोजन में निहित है। नियमित बैठकें पारस्परिक समर्थन के नेटवर्क बनाती हैं जो वित्तीय लेनदेन से कहीं अधिक विस्तृत होती हैं और इसमें बाल देखभाल सहयोग, नौकरी की जानकारी साझाकरण, और शहरी चुनौतियों के आसपास सामूहिक समस्या-समाधान शामिल है। हाशिए के समुदायों की महिलाओं के लिए, SHGs अक्सर औपचारिक संगठनात्मक भागीदारी और लोकतांत्रिक निर्णय लेने के साथ उनका पहला अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने SHG-आधारित दृष्टिकोण की स्केलिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। 2014-15 से 7.8 लाख से अधिक शहरी SHGs का गठन किया गया है, जिनमें से 5.36 लाख से अधिक को रिवॉल्विंग फंड सहायता मिली है। इन समूहों ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों के माध्यम से 7.17 लाख ऋण की सुविधा प्रदान की है, संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट पहुंच प्रदान करना जो व्यापार विकास और संपत्ति निर्माण को सक्षम बनाता है।
आर्थिक सहकारिताएं: जीवित रहने से समृद्धि तक
बुनियादी वित्तीय समावेशन से परे, हाशिए के शहरी समुदाय उत्पादन और सेवा सहकारिताएं विकसित कर सकते हैं जो उनके पारंपरिक कौशल को शहरी आर्थिक संपत्ति में बदल देती हैं। अमुल मॉडल एक टेम्प्लेट प्रदान करता है कि कैसे हाशिए के ग्रामीण उत्पादक आर्थिक सहकारिताएं बना सकते हैं जो बिचौलियों और मध्यस्थों को खोने के बजाय मूल्य को पकड़ती हैं।
शहरी हाशिए के समुदायों के लिए, आर्थिक सहकारिताओं में शामिल हो सकते हैं:
- हस्तशिल्प और कारीगर सहकारिताएं जो पारंपरिक कौशल को शहरी लक्जरी बाजारों से जोड़ती हैं
- खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताएं जो ग्रामीण कनेक्शन क्षेत्रों से कृषि उत्पादों में मूल्य जोड़ती हैं
- सेवा सहकारिताएं जो घरेलू कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों और अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिभागियों को संगठित करती हैं
- अपशिष्ट प्रबंधन सहकारिताएं जो अपशिष्ट संग्रह और पुनर्चक्रण गतिविधियों को औपचारिक बनाती हैं
- निर्माण सहकारिताएं जो शहरी विकास परियोजनाओं के लिए कुशल और अकुशल श्रम को संगठित करती हैं
स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) प्रदर्शित करता है कि कैसे व्यापक सहकारी दृष्टिकोण लोकतांत्रिक शासन बनाए रखते हुए हाशिए के कामगार स्थितियों को बदल सकते हैं। SEWA कृषि, उत्पादन, स्ट्रीट वेंडिंग और सेवाओं में 1.5 मिलियन सदस्यों को संगठित करता है, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और सदस्य सशक्तिकरण के साथ व्यवहार्य लोकतांत्रिक सहकारिताएं बनाता है।
आवास सहकारिताएं: शहरी आश्रय को सुरक्षित करना
आवास हाशिए के शहरी प्रवासियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, किराया बाजारों में भेदभाव के साथ अक्सर परिवारों को अपर्याप्त अनौपचारिक बस्तियों में मजबूर करता है। आवास सहकारिताएं शक्तिशाली विकल्प प्रदान करती हैं जो सामुदायिक संपत्ति बनाते हुए किफायती, सुरक्षित आवास प्रदान करती हैं।
सामूहिक स्वामित्व मॉडल सदस्यों को व्यक्तिगत कब्जे के अधिकारों को बनाए रखते हुए भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए संसाधन जमा करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण उन परिवारों के लिए घर का स्वामित्व सुलभ बनाता है जो स्वतंत्र रूप से शहरी आवास लागत वहन नहीं कर सकते। सफल आवास सहकारिताओं में, प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत इकाई और अंतर्निहित भूमि का आनुपातिक हिस्सा दोनों का मालिक होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समय के साथ संपत्ति प्रशंसा से लाभ उठाएं।
भारत के आवास सहकारी क्षेत्र में राज्यों में 26 एपेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन द्वारा समर्थित 191,955 से अधिक पंजीकृत सहकारिताएं शामिल हैं। राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ सहकारी विकास, तकनीकी सहायता और नीति वकालत के लिए संस्थागत समर्थन प्रदान करता है।
सामुदायिक भूमि ट्रस्ट हाशिए के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता के साथ एक उभरता हुआ मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। CLT व्यवस्था में, गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा भूमि को सामूहिक रूप से रखा जाता है जबकि इमारतें व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में होती हैं। यह सामुदायिक सदस्यों के लिए स्थायी सामर्थ्य सुनिश्चित करते हुए भूमि को सट्टा बाजारों से हटा देता है।
नीतिगत ढांचे और सरकारी सहायता
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सहायता प्रणालियां
भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के माध्यम से शहरी हाशिए के समुदायों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए व्यापक ढांचे विकसित किए हैं। यह कार्यक्रम शहरी गरीब परिवारों, बेघर व्यक्तियों और स्ट्रीट वेंडरों को लक्षित करता है स्थायी आजीविका बनाने और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हस्तक्षेपों के साथ।
रोजगार कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (EST&P) घटक ने 2014-15 से 13 लाख से अधिक शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, 6.78 लाख से अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिला है। यह स्केल्ड कार्यक्रमों की क्षमता का प्रदर्शन करता है जो हाशिए के समुदायों को औपचारिक क्षेत्र के अवसरों के साथ जोड़ते हैं जबकि उनकी शहरी आर्थिक क्षमताओं का निर्माण करते हैं।
PM SVANidhi योजना ने 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को कुल ₹13,797 करोड़ के 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए हैं, संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना जो व्यापार विस्तार और औपचारिकरण को सक्षम बनाता है। योजना का डिजिटल लेनदेन और वित्तीय साक्षरता पर जोर ₹6.09 लाख करोड़ मूल्य के 557 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन उत्पन्न कर चुका है, दिखाते हुए कि कैसे लक्षित समर्थन अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को औपचारिक आर्थिक प्रणालियों में एकीकृत कर सकता है।
व्यापक सामाजिक सुरक्षा एकीकरण
SVANidhi se Samriddhi Initiative प्रदर्शित करती है कि कैसे व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ सकता है। मासिक लोक कल्याण मेलों के माध्यम से, लाभार्थी आठ केंद्रीय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं, व्यापक समर्थन नेटवर्क बनाते हुए जो तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं से परे विस्तार करते हैं।
नया शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पायलट कार्यक्रम छह कमजोर व्यावसायिक समूहों पर केंद्रित है: निर्माण कामगार, परिवहन कामगार, गिग वर्कर्स, देखभाल कामगार, अपशिष्ट कामगार और घरेलू कामगार। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण हाशिए के शहरी प्रवासियों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार की वास्तविकता के साथ मेल खाता है और विशिष्ट सामुदायिक आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करता है।
चुनौतियां और निरंतर बाधाएं
निरंतर शहरी भेदभाव और पृथक्करण
नीतिगत ढांचों और संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, हाशिए के शहरी समुदाय आवास, रोजगार और सामाजिक सेवाओं में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना जारी रखते हैं। शोध निरंतर आवास भेदभाव का दस्तावेजीकरण करता है जहां योग्य दलित और मुस्लिम परिवार आर्थिक योग्यता के बजाय पहचान चिह्नकों के आधार पर अस्वीकार का सामना करते हैं। यह समुदायों को केंद्रित बस्तियों में मजबूर करता है जिनमें पर्याप्त अवसंरचना और सेवाओं की कमी हो सकती है।
रोजगार भेदभाव बाजार-संचालित और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रों में भी बना रहता है। ऑडिट अध्ययन दिखाते हैं कि कैसे हाशिए की पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवार योग्यता या क्षमता के बजाय जाति और धार्मिक पहचान के आधार पर भर्ती अस्वीकृति का सामना करते हैं। यह व्यावसायिक पृथक्करण आर्थिक गतिशीलता को सीमित करता है और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी को कायम रखता है।
विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में हाशिए के समुदायों की एकाग्रता, सामाजिक पूंजी प्रदान करते हुए, व्यापक शहरी अवसरों और सेवाओं से अलगाव भी पैदा कर सकती है। भौगोलिक पृथक्करण गरीबी को कायम रख सकता है और पीढ़ियों में सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकता है, ग्रामीण बहिष्करण के शहरी संस्करण बनाता है।
संस्थागत और कार्यान्वयन अंतराल
हाशिए के समुदायों की सेवा करने वाली कई सहकारिताएं संपार्श्विक आवश्यकताओं और दस्तावेजीकरण बाधाओं के कारण औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। पारंपरिक बैंकों को अक्सर गारंटी और औपचारिक कागजात की आवश्यकता होती है जो नवगठित सहकारिताएं प्रदान नहीं कर सकतीं, उनकी संचालन स्केल करने और सदस्य की आवश्यकताओं की प्रभावी रूप से सेवा करने की क्षमता को सीमित करता है।
उचित प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन के बिना शासन और प्रबंधन क्षमता की कमी सहकारी प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है। कई सहकारिताएं वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना और संघर्ष समाधान के साथ संघर्ष करती हैं, निरंतर क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है।
व्यापक नीतिगत ढांचों के बावजूद, कार्यान्वयन अक्सर नीतिगत इरादों से कम पड़ता है। नौकरशाही देरी, भ्रष्टाचार और सरकारी स्तरों के बीच समन्वय विफलताएं कार्यक्रम प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं और इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने वाले वास्तविक लाभों को कम कर सकती हैं।
सफलता की कहानियां और परिवर्तनकारी मॉडल
मुक्ति की व्यक्तिगत कहानियां
बुंदेलखंड की एक दलित महिला नेता प्रीति की कहानी दिखाती है कि कैसे रणनीतिक शहरी जुड़ाव नेतृत्व के अवसर पैदा कर सकता है जो ग्रामीण सेटिंग में असंभव होते। जब COVID-19 के दौरान 85 दलित प्रवासी परिवार बीजापुर वापस आए और प्रभुत्वशाली जातियों से बहिष्करण का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें गांव में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया, प्रीति ने राहत प्रयासों का आयोजन किया जो स्वास्थ्य शिविर, सूखा राशन, और सरकारी स्कूलों में आश्रय प्रदान करता था।
स्थानीय अधिकारियों के साथ अपनी निरंतर वकालत और राहत प्रयासों के व्यवस्थित संगठन के माध्यम से, प्रीति 87 से अधिक परिवारों के लिए MGNREGA रोजगार, 15 वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन, और तीन गांवों में 150 लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन सुरक्षित करने में सक्षम थी। उसकी सफलता दिखाती है कि कैसे शहरी-शिक्षित हाशिए के व्यक्ति स्थायी आजीविका बनाते हुए ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं।
शहरी गुमनामी और व्यावसायिक सफलता
शोध दस्तावेजित करता है कि कैसे शहरी वातावरण हाशिए के व्यक्तियों को व्यावसायिक पहचान बनाने की अनुमति देता है जो ग्रामीण जाति सीमाओं से परे होती है। अजय नवारिया के संकलन की चुनी गई कहानियां दिखाती हैं कि कैसे शहरी दलित पुरुष शहर की गुमनामी का लाभ उठाकर करियर और रिश्ते बनाते हैं जो ग्रामीण संदर्भों में असंभव होते। शहर की गुमनामी द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता व्यक्तियों को पारंपरिक जाति-बाध्य व्यवसायों से परे क्षमताओं और आकांक्षाओं को विकसित करने में सक्षम बनाती है।
पोखरा, नेपाल के एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी दलित समुदायों ने अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में मजबूत सामूहिक पहचान और अधिक प्रभावी वकालत क्षमताएं विकसित कीं। शहरी वातावरण ने शिक्षा, संगठनात्मक भागीदारी और राजनीतिक जुड़ाव के अवसर प्रदान किए जिन्होंने अधिकार मुखरता और सामूहिक कार्रवाई के लिए सामुदायिक क्षमता को मजबूत किया।
सामूहिक संगठन और समुदायिक निर्माण
दिल्ली की स्क्वाटर बस्तियां दिखाती हैं कि कैसे हाशिए के शहरी प्रवासी “कॉस्मोपॉलिटन पड़ोसीपन” बना सकते हैं जो विविध सामुदायिक पृष्ठभूमि को जोड़ता है। केवल ग्रामीण सामाजिक पदानुक्रमों को दोहराने के बजाय, ये बस्तियां पारस्परिक समर्थन और सहयोग के नए रूप बनाती हैं जो विविध सामुदायिक शक्तियों पर आधारित होते हैं।
शहरी झुग्गियों में जाति, धर्म और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का मिश्रण ऐसी सामाजिक गतिकी बनाता है जो ग्रामीण पृथक गांवों में असंभव होती। जबकि चुनौतियां निश्चित रूप से मौजूद हैं, यह विविधता सीखने, पारस्परिक समर्थन और सामूहिक कार्रवाई के अवसर भी बनाती है जो समग्र सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत कर सकती है।
समुदायिक सशक्तिकरण के लिए रणनीतिक सिफारिशें
एकीकृत प्रवासन रणनीतियों का विकास
ग्रामीण उत्पीड़न का सामना कर रहे समुदायों को शहरी अवसरों तक पहुंचते हुए सुरक्षात्मक नीतियों तक पहुंच बनाए रखने के लिए अपने गृह राज्यों के भीतर निकटवर्ती शहरी गंतव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण परिवारों को आरक्षण लाभ, शैक्षणिक पहुंच और कल्याणकारी कार्यक्रम पात्रता बनाए रखने की अनुमति देता है जबकि शहरी आजीविका और क्षमताओं का निर्माण करता है।
पूर्व-प्रवासन योजना में संभावित गंतव्य शहरों में मौजूदा सामाजिक नेटवर्क, सहकारी संगठनों और समर्थन प्रणालियों की पहचान शामिल होनी चाहिए। समुदाय प्रवासन शुरू करने से पहले संसाधनों की पहचान करने और बसावट रणनीति विकसित करने के लिए दिशा फाउंडेशन और अन्य प्रवासी समर्थन समूहों जैसे संगठनों से संपर्क कर सकते हैं।
चक्रीय प्रवासन दृष्टिकोण परिवारों को जोखिम कम करते हुए क्रमिक संक्रमण को सक्षम बनाते हुए शहरी क्षमताओं का निर्माण करते समय ग्रामीण संबंध बनाए रखने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण आर्थिक विविधीकरण और जोखिम शमन प्रदान करता है जबकि परिवारों को चल रहे उत्पीड़न का सामना कर रहे ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का समर्थन करने की अनुमति देता है।
व्यापक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
सफल शहरी एकीकरण के लिए वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक सहकारिताओं के समन्वित विकास की आवश्यकता होती है जो सामुदायिक आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला को संबोधित करते हैं। समुदायों को अलग-थलग एकल-उद्देश्य संगठनों के बजाय एकीकृत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का लक्ष्य रखना चाहिए जो सदस्य सशक्तिकरण के लिए व्यापक समर्थन प्रदान कर सके।
छोटे SHGs से बड़ी आर्थिक सहकारिताओं तक प्रगतिशील स्केलिंग समुदायों को लोकतांत्रिक शासन बनाए रखते हुए संगठनात्मक क्षमता को धीरे-धीरे बनाने की अनुमति देती है। बुनियादी बचत समूहों से बैंक-लिंक्ड क्रेडिट पहुंच से औपचारिक सहकारी उद्यमों तक की प्रगति स्थायी विकास के लिए एक सिद्ध मार्ग प्रदर्शित करती है।
प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सहकारी विकास रणनीतियों के मुख्य घटक होने चाहिए। आधुनिक सहकारिताओं को शहरी बाजारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन और ग्राहक जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहिए।
वकालत और राजनीतिक भागीदारी
सहकारी संगठनों को स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी विकास नीतियां हाशिए के समुदाय के हितों का समर्थन करती हैं। इसमें शहर नियोजन प्रक्रियाओं में भाग लेना, समावेशी ज़ोनिंग नीतियों की वकालत करना, और हाशिए के समुदाय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना शामिल है।
भेदभाव के मामलों का दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग नीति वकालत और कानूनी कार्रवाई के लिए साक्ष्य आधार बनाने में मदद करता है। समुदायों को भेदभाव और हिंसा के मामलों का दस्तावेजीकरण करने और कानूनी उपचार करने के लिए सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठनों के साथ काम करना चाहिए।
अन्य हाशिए के शहरी समुदायों के साथ गठबंधन निर्माण सामूहिक वकालत शक्ति और संसाधन साझाकरण को मजबूत कर सकता है। SEWA मॉडल प्रदर्शित करता है कि कैसे व्यावसायिक और सामुदायिक सीमाओं के पार संगठन अधिक प्रभावी वकालत और सेवा वितरण बना सकता है।
निष्कर्ष: ग्रामीण उत्पीड़न से शहरी सशक्तिकरण तक
अपने ग्रामीण जन्मस्थानों में अमानवीय व्यवहार का सामना कर रहे उत्पीड़ित और दलित समुदायों के लिए, सहकारी नेटवर्क विकास के साथ मिलकर रणनीतिक शहरी प्रवासन केवल एक भागने का रास्ता नहीं बल्कि गरिमा, सशक्तिकरण और स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। ग्रामीण उत्पीड़न की क्रूर वास्तविकताएं—आकस्मिक हिंसा से लेकर व्यवस्थित आर्थिक शोषण तक—शहरी प्रवासन को अस्तित्व और मानव गरिमा के लिए एक विकल्प से कम और आवश्यकता अधिक बनाती हैं।
साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि जबकि शहर जाति-आधारित भेदभाव के लिए रामबाण नहीं हैं, वे गुमनामी, आर्थिक विविधीकरण और सामूहिक संगठन के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं जो ग्रामीण संदर्भों में असंभव रहते हैं। मुक्ति के स्थानों के रूप में शहरों का डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, भले ही शहरी भेदभाव नवाचार प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाली नई चुनौतियां पैदा करता है।
सफल परिवर्तन की कुंजी सामूहिक सशक्तिकरण रणनीतियों के साथ व्यक्तिगत प्रवासन निर्णयों के रणनीतिक एकीकरण में निहित है। समुदायों को पारस्परिक समर्थन, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक वकालत क्षमताएं प्रदान करने वाले सहकारी नेटवर्क का निर्माण करते हुए शहरी गुमनामी और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों, आवास सहकारिताओं, आर्थिक उद्यमों और व्यापक सामाजिक समर्थन प्रणालियों के माध्यम से, हाशिए के शहरी समुदाय स्थायी आजीविका बना सकते हैं जो गरिमा और समृद्धि प्रदान करती हैं।
सफलता के लिए समुदायों स्वयं से समन्वित कार्रवाई, सहायक सरकारी नीतियां और इन समुदायों द्वारा शहरी समृद्धि में दिए गए योगदान की व्यापक सामाजिक मान्यता की आवश्यकता होती है। जो शहर समुदाय-संचालित विकास दृष्टिकोणों को अपनाते और समर्थन करते हैं, वे उद्यमिता, कौशल और लचीलेपन से लाभान्वित होते हैं जो हाशिए के समुदाय शहरी अर्थव्यवस्थाओं में लाते हैं। जो ऐसा समर्थन प्रदान करने में विफल रहते हैं, वे शहरी गरीबी, सामाजिक तनाव और आर्थिक अक्षमता की बढ़ती समस्याओं का सामना करेंगे।
ग्रामीण उत्पीड़न से शहरी सशक्तिकरण तक का रास्ता न तो सरल है और न ही गारंटीशुदा, लेकिन यह व्यवस्थित उत्पीड़न से बचने के साथ-साथ टिकाऊ भविष्य बनाने की चाह रखने वाले समुदायों के लिए उपलब्ध सबसे व्यावहारिक रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। रणनीतिक बसावट, सहकारी संगठन और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से, उत्पीड़ित समुदाय वास्तव में अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं और भारत के शहरी भविष्य में समान प्रतिभागियों के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकते हैं।
यात्रा में साहस, योजना और एकजुटता की आवश्यकता होती है, लेकिन विकल्प—ग्रामीण हिंसा और अमानवीयकरण की निरंतर अधीनता—जोखिमों को सार्थक बनाता है। ग्रामीण उत्पीड़न के चक्रों में फंसे उन समुदायों के लिए, शहर केवल आर्थिक अवसर नहीं बल्कि मानव गरिमा के मौलिक वादे और जन्म के बजाय क्षमता के आधार पर जीवन निर्माण की संभावना प्रदान करते हैं। उचित सहकारी नेटवर्क और नीतिगत ढांचों द्वारा समर्थित यह परिवर्तन व्यक्तिगत मुक्ति और भारत के व्यापक लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास में योगदान दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।