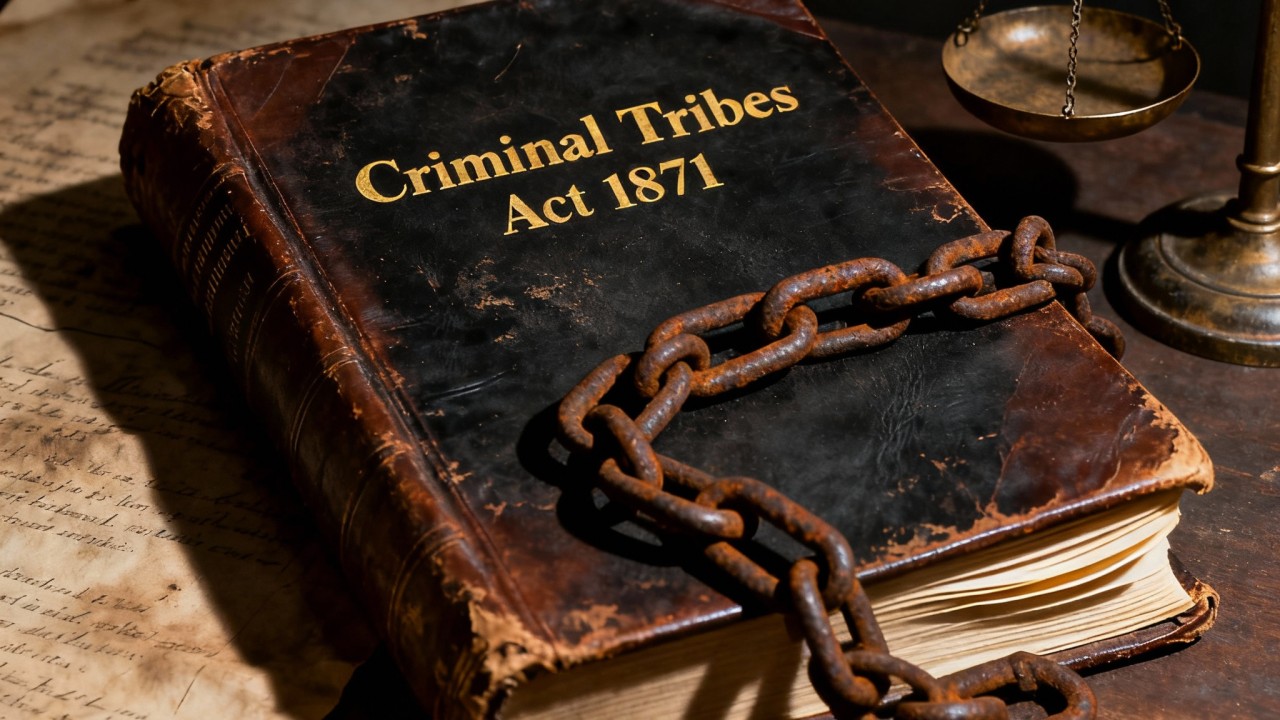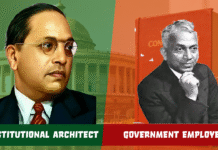1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम: औपनिवेशिक कानूनी इतिहास का एक काला अध्याय
1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किए गए सबसे कठोर और भेदभावपूर्ण कानूनों में से एक है। इस अधिनियम ने वंशानुगत अपराध की अभूतपूर्व अवधारणा को जन्म देकर, पूरे समुदायों को “जन्मजात अपराधी” करार देकर और लाखों भारतीयों को व्यवस्थित निगरानी, जबरन बसने और सामाजिक बहिष्कार के अधीन करके कानूनी परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय, 127 समुदायों के 30 लाख लोग इस औपनिवेशिक कानून की छाया में थे। इस अधिनियम की विरासत 1949 में इसके औपचारिक निरसन से कहीं आगे तक फैली हुई है, क्योंकि विमुक्त जनजातियाँ समकालीन भारत में भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना जारी रखती हैं, जो स्वतंत्रता के बाद के समाज पर औपनिवेशिक कानूनी ढाँचों के स्थायी प्रभाव को उजागर करता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति
पूर्व-औपनिवेशिक पृष्ठभूमि और जातिगत पदानुक्रम
आपराधिक जनजाति अधिनियम की नींव प्राचीन भारतीय सामाजिक पदानुक्रमों में निहित है, जिनका बाद में औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा शोषण और कठोरता से उपयोग किया गया। ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों ने जाति-आधारित भेद स्थापित किए थे, जिससे भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न हुआ। हालाँकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने इन पारंपरिक सामाजिक श्रेणियों को नियंत्रण और शासन के प्रशासनिक उपकरणों में बदल दिया। भारतीय समाज की स्वाभाविक रूप से अराजक होने की औपनिवेशिक व्याख्या ने असाधारण कानूनी उपायों के लिए वैचारिक औचित्य प्रदान किया। ब्रिटिश वायसराय की परिषद के एक सदस्य ने 1860 के दशक में कहा था कि भारत एक “पूरी तरह से कानूनविहीन” राष्ट्र है, और जानबूझकर उन जटिल पारंपरिक कानूनी प्रणालियों की अनदेखी की जो सदियों से भारतीय समुदायों पर शासन करती आ रही थीं।
ठगी की मिसाल
आपराधिक जनजाति अधिनियम की तात्कालिक कानूनी मिसाल 1830 के दशक में ठगी के खिलाफ ब्रिटिश अभियान से उभरी। 1836-48 के ठगी और डकैती दमन अधिनियमों ने सामूहिक अपराध के क्रांतिकारी कानूनी सिद्धांत की स्थापना की, जिसके तहत व्यक्तियों को व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि के साक्ष्य के बिना केवल समूह संबद्धता के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता था। मेजर जनरल विलियम एच. स्लीमन ने इस अभियान का नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा संगठित आपराधिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित की जाने वाली व्यवस्था के बारे में व्यापक ज्ञान विकसित किया। ठगी के दमन ने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जो विशिष्ट समूहों के भीतर वंशानुगत आपराधिक प्रवृत्तियों को मानता था, जिसने आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इस सिद्धांत के व्यापक अनुप्रयोग के लिए आधार तैयार किया।
1857 के विद्रोह के बाद
आपराधिक जनजाति अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद की स्थिति की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया, जहाँ कई आदिवासी सरदारों को देशद्रोही और विद्रोही करार दिया गया था। इस विद्रोह ने खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश आबादी पर ब्रिटिश नियंत्रण की कमज़ोरी को उजागर कर दिया था, जो तेज़ी से संगठित हो सकते थे और पारंपरिक निगरानी विधियों से बच सकते थे। औपनिवेशिक प्रशासक इन गतिशील समुदायों को ब्रिटिश शासन की स्थिरता के लिए स्वाभाविक रूप से ख़तरा मानते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की: विद्रोह के संभावित स्रोतों का दमन, कराधान और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाना, और ब्रिटिश औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय समाज को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई सामाजिक इंजीनियरिंग परियोजनाओं को लागू करना।
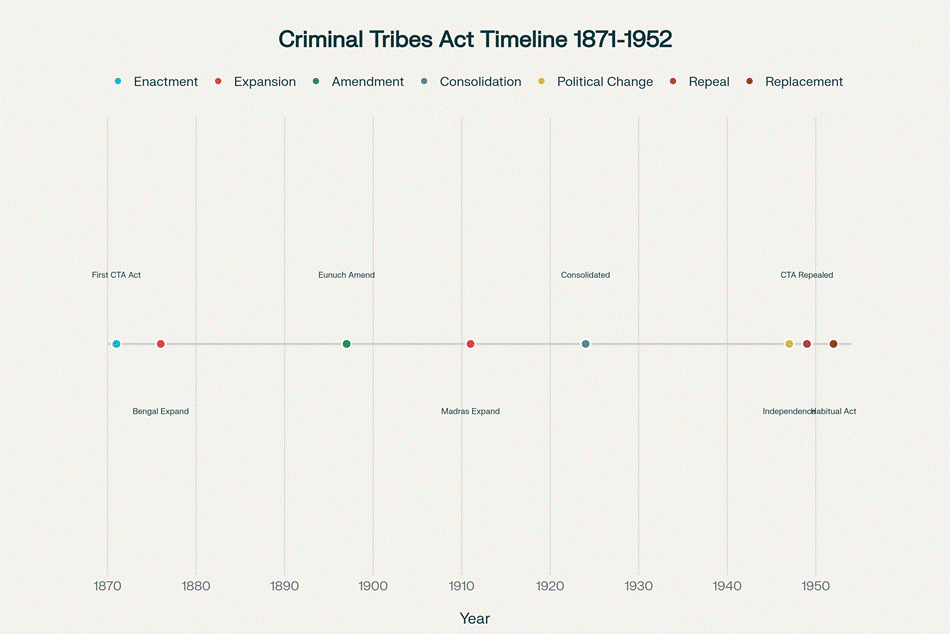
कानूनी ढांचा और प्रावधान
मुख्य विधायी संरचना
1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम 12 अक्टूबर, 1871 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में छह विशिष्ट विशेषताएँ थीं जो इसे सामान्य आपराधिक कानून से अलग करती थीं। पहला, यह सामान्य दंडात्मक कानून से ऊपर था, और उन कृत्यों के लिए प्रतिबंध और दंड निर्धारित करता था जो मानक कानूनी ढाँचों के तहत सामान्यतः आपराधिक अपराध नहीं माने जाते थे। दूसरा, यह संपूर्ण जनजातियों, गिरोहों या व्यक्तियों के उन वर्गों पर लागू होता था जिनके बारे में स्थानीय सरकारों का दावा था कि वे “गैर-जमानती अपराधों को व्यवस्थित रूप से करने के आदी” हैं। इस व्यापक अनुप्रयोग का अर्थ था कि व्यक्तिगत निर्दोषता या अपराध अप्रासंगिक हो गए; किसी निर्दिष्ट समूह की सदस्यता ही कानूनी प्रतिबंधों के लिए पर्याप्त थी।
अधिसूचना और निगरानी तंत्र
अधिनियम की धारा 3 के तहत, स्थानीय अधिकारियों के पास किसी भी समूह को “जमानत द्वारा दंडनीय नहीं होने वाले अपराध करने की व्यवस्थित लत” वाले किसी भी समूह को आपराधिक जनजाति के रूप में चिह्नित करने की शक्ति थी। एक बार अधिसूचित होने के बाद, इन समुदायों को व्यापक निगरानी उपायों का सामना करना पड़ा, जिसमें अनिवार्य हाजिरी, पासपोर्ट प्रणाली के माध्यम से प्रतिबंधित आवाजाही और कई अन्य कानूनी अक्षमताएँ शामिल थीं। अधिनियम ने यह स्थापित किया कि “ऐसी प्रत्येक अधिसूचना इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि इस अधिनियम के प्रावधान उसमें निर्दिष्ट जनजाति, गिरोह या वर्ग पर लागू होते हैं,” जिससे कानूनी चुनौती या न्यायिक समीक्षा की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया। इस प्रावधान ने प्रभावित समुदायों को प्रभावी रूप से सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के संरक्षण से बाहर कर दिया।
पंजीकरण और आवागमन नियंत्रण
अधिनियम ने अधिसूचित जनजातियों के सभी वयस्क पुरुष सदस्यों के लिए व्यापक पंजीकरण आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया। धारा 10(1)(क) के तहत ग्राम पुलिस थानों या पंचायतों को बच्चों और आश्रितों सहित प्रत्येक घर के सभी वयस्क पुरुषों के नाम, बाएँ अंगूठे के निशान और आयु वाले रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता थी। प्रत्येक पंजीकृत सदस्य को साप्ताहिक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित अनुसार पुलिस या ग्राम प्रशासन को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया था, जिससे उनकी आवागमन की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर गंभीर प्रतिबंध लग गया। निवास बदलने वाले किसी भी पंजीकृत सदस्य को तुरंत ग्राम प्रधान को अपने स्थायी और अस्थायी दोनों पतों की सूचना देनी होती थी, और सभी परिवर्तनों को ग्राम रजिस्ट्री में दर्ज करना होता था।
सुधारात्मक बस्तियाँ और जबरन श्रम
अधिनियम की धारा 6 ने सरकार को आपराधिक जनजाति के सदस्यों के लिए विशेष “सुधारात्मक बस्तियाँ” स्थापित करने का अधिकार दिया, जो जबरन पुनर्वास केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं। पूरे परिवारों को इकट्ठा करके दूर-दराज, एकांत स्थानों पर ले जाया जाता था जो खुली जेलों की तरह काम करते थे। इन बस्तियों में, लोगों को औद्योगिक या कृषि कार्यों के माध्यम से सुधार की आड़ में जबरन श्रम कराया जाता था। मद्रास प्रेसीडेंसी में, अधिसूचित जनजातियों के सदस्यों को यरवदा सुधारात्मक केंद्र जैसी सुविधाओं में ले जाया जाता था, जहाँ वे बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित रहते हुए निरंतर निगरानी में काम करते थे। इन बस्तियों ने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की, एक तो संभावित खतरों को नियंत्रित किया और साथ ही औपनिवेशिक उद्यमों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराया।
कार्यान्वयन और विस्तार
भौगोलिक विस्तार
आपराधिक जनजाति अधिनियम को शुरू में ब्रिटिश भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लागू किया गया था, जिसके बाद इसे पूरे उपमहाद्वीप में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। 1876 में इस अधिनियम का विस्तार बंगाल तक किया गया और धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ। 1911 में मद्रास प्रेसीडेंसी इसे लागू करने वाला अंतिम राज्य बना। इस चरणबद्ध विस्तार ने औपनिवेशिक प्रशासकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और निगरानी एवं नियंत्रण की अधिकाधिक परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने का अवसर दिया। 1924 तक, यह अधिनियम कई संशोधनों और समेकनों के माध्यम से औपनिवेशिक भारत के अधिकांश हिस्सों में लागू हो चुका था, जिससे इसका दायरा और गंभीरता बढ़ गई।
प्रशासनिक कार्यान्वयन
ग्राम प्रधानों और पुलिस अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारियों को यह निर्धारित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गईं कि किन व्यक्तियों और समुदायों को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। इस विनियमन के तहत स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक व्यक्ति की व्यापक सूची तैयार करनी होती थी। एक बार किसी व्यक्ति का नाम ऐसी सूची में आ जाने पर, उसे हटाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, जिससे स्थायी वर्गीकरण बन गया जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहा। इस अधिनियम ने किसी अधिकारी के निर्णयों को कानूनी चुनौतियों से विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया, यहाँ तक कि प्रशासनिक शक्ति पर प्रतीकात्मक नियंत्रण और संतुलन को भी समाप्त कर दिया।
समुदाय लक्ष्यीकरण और दायरा
अपने चरम कार्यान्वयन तक, आपराधिक जनजाति अधिनियम ने भारत भर के सैकड़ों समुदायों को प्रभावित किया। औपनिवेशिक सरकार ने 1931 तक अकेले मद्रास प्रेसीडेंसी में इस अधिनियम के तहत 237 आपराधिक जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया। शुरुआत में गुज्जर, हरनी (राजपूत का एक उप-वंश) और लोधी समुदायों जैसे समूहों को लक्षित करते हुए, इस अधिनियम का प्रवर्तन 19वीं शताब्दी के अंत तक विस्तारित हो गया और इसमें अधिकांश शूद्र और चमार जैसे “अछूत”, साथ ही सन्यासी और पहाड़ी जनजातियाँ भी शामिल हो गईं। इस अधिनियम ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदायों को भी लक्षित किया, 1897 के संशोधन ने इसके दायरे में किन्नरों को भी जोड़ा और आदेश दिया कि “आपराधिक” किन्नर “सार्वजनिक सड़क पर महिलाओं की तरह कपड़े पहने या अलंकृत… बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाएँ” और जेल में डाले जाएँ।
| Community/Tribe | Region/State | Traditional Occupation | Current Status |
|---|---|---|---|
| Gujjars | North India (Punjab, Haryana) | Pastoralism, Trading | Denotified – mostly OBC |
| Chamars | North India (UP, Bihar) | Leatherwork, Agriculture | Denotified – SC |
| Sansis | Punjab, Haryana | Trading, Performance | Denotified – OBC |
| Bhils | Central India (MP, Gujarat) | Agriculture, Forest Work | Mostly ST |
| Pardhis | Central India (MP, Maharashtra) | Hunting, Gathering | Denotified – struggling |
| Banjaras/Lambadas | South India (Karnataka, Telangana) | Trading, Cattle Rearing | Denotified – ST/OBC |
| Narikuravars | Tamil Nadu | Beadwork, Street Vending | Denotified – no ST status |
| Ahirs | North India (Rajasthan, UP) | Pastoralism | Denotified – OBC |
| Lodhi | Central India (MP, UP) | Agriculture, Trading | Denotified – OBC |
| Sanyasis | Across India | Religious Mendicancy | Denotified |
| Domes | Bengal | Scavenging, Manual Labor | Denotified – SC |
| Rebari | Rajasthan, Gujarat | Pastoralism | Denotified – OBC |
| Bhar | North India | Agriculture | Denotified |
| Pasi | North India | Agriculture, Labor | Denotified – SC |
| Yerukula | South India | Basket Making | Denotified |
| Bedia | Central India | Folk Performance | Denotified – struggling |
| Chharas | Gujarat | Street Performance | Denotified – ongoing stigma |
| Kanjars | North India | Trading | Denotified |
| Tadvis | Central India | Labor | Denotified |
| Nat | Across India | Performance, Acrobatics | Denotified |
| Irula | South India | Snake Catching | Denotified |
| Bowreah | Bengal | Trading | Denotified |
| Budducks | Bengal | Labor | Denotified |
| Bedyas | Bengal | Labor | Denotified |
प्रभावित समुदायों पर प्रभाव
सामाजिक कलंक और हाशिए पर डालना
“आपराधिक जनजातियों” के पदनाम ने सामाजिक कलंक की एक अमिट छाप छोड़ी जो कानूनी प्रतिबंधों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। यही पदनाम समकालीन पर्यवेक्षकों द्वारा “कैन का चिह्न” के रूप में वर्णित किया जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक समाज से सामाजिक बहिष्कार और भी गहरा गया। उच्च जाति और गैर-अधिसूचित पड़ोसी इन समुदायों को अधिक संदेह और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, यह जानते हुए कि सरकार ने स्वयं उन्हें वंशानुगत अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया था। 1880 के दशक में लिखते हुए ब्रिटिश मिशनरियों ने देखा कि जब आपराधिक जनजातियों के सदस्यों ने बसने और ईमानदारी से रहने का प्रयास किया, तब भी ग्रामीणों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्हें उपहासपूर्वक “सीटीए-वाला” कहा और अक्सर उन्हें सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच से वंचित कर दिया।
आर्थिक व्यवधान और दरिद्रता
अधिनियम के आवागमन प्रतिबंधों ने कई प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से खानाबदोश व्यापार और मौसमी प्रवास पर निर्भर समुदायों की आर्थिक नींव को तहस-नहस कर दिया। पारंपरिक कारवां व्यापारी, लम्बाडा/बंजारा लोगों ने, जब गतिशीलता में कटौती की गई, तो अपने व्यापक व्यापार नेटवर्क खो दिए और उन्हें ऐसी बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जहाँ सार्थक काम दुर्लभ था। इसी प्रकार, पंजाब के सांसी, जो प्रदर्शन और छोटे-मोटे व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें सुधारक बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया और औपनिवेशिक निगरानी में शारीरिक श्रम करने पर मजबूर कर दिया गया। पहले से मौजूद जातिगत भेदभाव के कारण कई समुदायों के पास न्यूनतम भूमि स्वामित्व था, और उनके पास जो भी भूमि या संपत्ति थी, उसे अक्सर जबरन पुनर्वास के दौरान जब्त कर लिया जाता था।
सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक प्रथाओं का विनाश
खानाबदोश समुदायों के जबरन बसने के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का व्यवस्थित विनाश हुआ। जिन समुदायों ने पीढ़ियों से मौखिक परंपराओं, मौसमी त्योहारों और विशिष्ट शिल्पों को बनाए रखा था, उनका सांस्कृतिक संचरण निगरानी आवश्यकताओं और भौगोलिक सीमाओं के कारण बाधित हुआ। बच्चों को अक्सर उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था और सुधारक संस्थाओं में रखा जाता था, जिससे सांस्कृतिक ज्ञान और पारंपरिक कौशल का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण बाधित होता था। औपनिवेशिक परिभाषाओं के अनुसार इन समुदायों को “उत्पादक” श्रमिकों में बदलने पर अधिनियम के जोर ने पारंपरिक व्यवसायों और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ उनके संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया।
शारीरिक कष्ट और मानवाधिकार उल्लंघन अधिनियम के तहत स्थापित सुधारक बस्तियों में निवासियों को कठोर शारीरिक परिस्थितियों और व्यवस्थित मानवाधिकारों के हनन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने विशेष बस्तियाँ स्थापित कीं जहाँ लोगों को “ऊँची दीवारों से घेरकर कैद, बेड़ियों में जकड़ा, बेंत से पीटा और कोड़े मारे जाते थे”। वयस्क पुरुषों को साप्ताहिक रूप से पुलिस थानों में रिपोर्ट करना अनिवार्य था, जबकि पूरे परिवार पर लगातार नज़र रखी जाती थी और आवाजाही संबंधी प्रतिबंधों के किसी भी कथित उल्लंघन के लिए बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। स्थायी संदेह और निगरानी में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने स्थायी आघात पैदा किया जिसने प्रभावित समुदायों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।
कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ
उचित प्रक्रिया का अभाव
आपराधिक जनजाति अधिनियम, मूलभूत कानूनी सुरक्षाओं को समाप्त करके, उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता था। अधिनियम का यह प्रावधान कि किसी समूह को अपराधी घोषित करना “निर्णायक प्रमाण” माना जाता है, का अर्थ था कि प्रभावित व्यक्तियों के पास न्यायिक समीक्षा या कानूनी चुनौती का कोई सहारा नहीं था। स्थापित कानूनी मानदंडों से इस असाधारण विचलन का अर्थ था कि पूरे समुदाय को अपने वर्गीकरण को चुनौती देने या सामान्य कानूनी माध्यमों से निवारण प्राप्त करने का कोई अवसर दिए बिना ही कठोर प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता था। इस प्रकार, अधिनियम ने एक समानांतर कानूनी प्रणाली का निर्माण किया जिसने संवैधानिक सुरक्षाओं को दरकिनार कर दिया और प्रशासनिक हिरासत और सामूहिक दंड के लिए मिसालें स्थापित कीं।
व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन
वंशानुगत आपराधिकता की धारणा ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत स्वायत्तता के सिद्धांतों का मूल रूप से उल्लंघन किया, जो आधुनिक कानूनी प्रणालियों का आधार बने। आपराधिक प्रवृत्ति को एक वंशानुगत विशेषता मानकर, अधिनियम ने व्यक्तिगत सुधार या चुनाव की संभावना को नकार दिया, जिससे मानव व्यवहार का एक नियतिवादी दृष्टिकोण निर्मित हुआ जो आपराधिक न्याय की विकसित होती समझ के विपरीत था। साप्ताहिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, आवाजाही प्रतिबंधों और निगरानी उपायों ने संघ, आवाजाही और निजता की बुनियादी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया, जिन्हें दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों में मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दी जाने लगी थी।
औपनिवेशिक कानूनी नवाचार
यह अधिनियम स्थायी निगरानी और नियंत्रण के लिए एक ऐसा ढाँचा तैयार करके औपनिवेशिक कानूनी रणनीति में एक महत्वपूर्ण नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है जो पारंपरिक आपराधिक कानून से कहीं आगे तक फैला हुआ है। विशिष्ट कृत्यों पर प्रतिक्रिया देने वाले पारंपरिक आपराधिक कानूनों के विपरीत, आपराधिक जनजाति अधिनियम ने स्वाभाविक रूप से खतरनाक मानी जाने वाली पूरी आबादी को नियंत्रित करके संभावित अपराधों को रोकने का प्रयास किया। आपराधिक न्याय के प्रति इस निवारक दृष्टिकोण ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो पूरे औपनिवेशिक काल और उसके बाद भी पुलिसिंग रणनीतियों और सुरक्षा कानूनों को प्रभावित करते रहे।
प्रतिरोध और विरोध
सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ
कठोर प्रतिबंधों और निगरानी के बावजूद, कई प्रभावित समुदायों ने औपनिवेशिक नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध और अनुकूलन की रणनीतियाँ विकसित कीं। कुछ समूहों ने आपराधिक जनजाति सूची से हटाए जाने के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों से याचिका दायर करने का प्रयास किया, हालाँकि अधिनियम के प्रावधानों ने ऐसी अपीलों को कानूनी रूप से असंभव बना दिया था। अन्य समूहों ने सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए निगरानी से बचने के लिए अपनी पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव करने का प्रयास किया। इन प्रतिक्रियाओं की जटिलता प्रभावित समुदायों द्वारा व्यवस्थित उत्पीड़न के बावजूद भी बनाए रखी गई एजेंसी को प्रदर्शित करती है।
प्रारंभिक सुधार आंदोलन
1930 और 1940 के दशक तक, अधिनियम के अन्याय के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण भारतीय राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों की आलोचना में वृद्धि हुई। 1937 में बॉम्बे सरकार द्वारा नियुक्त आपराधिक जनजाति अधिनियम जाँच समिति ने अधिनियम के दंडात्मक तत्वों को महत्वपूर्ण रूप से कमज़ोर करने की सिफ़ारिश की, यह मानते हुए कि यह कानून अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है और इससे भारी सामाजिक नुकसान हुआ है। अधिनियम की विफलताओं की इन आधिकारिक स्वीकृतियों ने अंततः इसके निरसन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।
अंतर्राष्ट्रीय आलोचना
मानव अधिकारों और व्यक्तिगत गरिमा की वैश्विक समझ विकसित होने के साथ ही, आपराधिक जनजाति अधिनियम में निहित वंशानुगत अपराध की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाँच के दायरे में आ गई। इस अधिनियम में वंशानुगत आपराधिक प्रवृत्तियों की जो धारणा थी, वह उभरते अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों और मानव व्यवहार की वैज्ञानिक समझ के विपरीत थी, जिससे औपनिवेशिक प्रशासनिक हलकों में भी इसका बचाव करना मुश्किल हो गया।
निरसन और परिणाम
निरस्तीकरण का मार्ग
आपराधिक जनजाति अधिनियम को अंततः अगस्त 1949 में निरस्त कर दिया गया, जो कि 1949-50 की आपराधिक जनजाति जाँच समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद हुआ। नव-स्वतंत्र भारत सरकार ने माना कि यह अधिनियम समानता और व्यक्तिगत अधिकारों के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ मौलिक रूप से असंगत था। औपचारिक निरसन प्रक्रिया में पहले से वर्गीकृत सभी आपराधिक जनजातियों को “अधिसूचित” करना शामिल था, जिससे आधिकारिक तौर पर वंशानुगत अपराधियों के रूप में उनका कानूनी पदनाम हटा दिया गया। हालाँकि, औपनिवेशिक से उत्तर-औपनिवेशिक कानूनी ढाँचे में परिवर्तन केवल भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने से कहीं अधिक जटिल साबित हुआ।
आदतन अपराधी अधिनियम, 1952
आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के बावजूद, भारत सरकार ने जल्द ही आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 लागू किया, जो विभिन्न कानूनी शब्दावली के तहत उन्हीं समुदायों को लक्षित करता रहा। समूह की सदस्यता के बजाय व्यक्तिगत व्यवहार पर आधारित होने के बावजूद, आदतन अपराधी अधिनियम ने गैर-अधिसूचित जनजातियों को असमान रूप से प्रभावित किया और अपने पूर्ववर्ती अधिनियम की कई निगरानी और नियंत्रण व्यवस्थाओं को बरकरार रखा। इस अधिनियम ने पुलिस से संदिग्धों की “आपराधिक प्रवृत्तियों” की जाँच करने और यह पता लगाने को कहा कि क्या उनका व्यवसाय “स्थिर जीवन शैली के अनुकूल” है, इस भाषा ने खानाबदोश और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ औपनिवेशिक युग के भेदभाव को प्रभावी ढंग से जारी रखा।
लगातार भेदभाव और समकालीन चुनौतियाँ
आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के सात दशक से भी अधिक समय बाद, गैर-अधिसूचित जनजातियों को व्यवस्थित भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ रहा है। कई पुलिस प्रशिक्षण नियमावलियों में अभी भी कुछ समुदायों को डिफ़ॉल्ट रूप से अपराधों के संदिग्ध के रूप में पहचाना जाता है, जो कानून प्रवर्तन प्रथाओं में औपनिवेशिक युग के पूर्वाग्रहों को कायम रखता है। इन समुदायों से जुड़ा सामाजिक कलंक अभी भी कायम है, जिससे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुँच प्रभावित होती है। समकालीन चुनौतियों में उचित दस्तावेज़ीकरण और पहचान पत्रों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच, आदतन अपराधी कानूनों के तहत निरंतर पुलिस उत्पीड़न और ऐतिहासिक रूढ़ियों के आधार पर चल रहा सामाजिक बहिष्कार शामिल है।
समकालीन प्रासंगिकता और चल रहे मुद्दे
वर्तमान कानूनी स्थिति और अधिकार
आज, भारत में 313 खानाबदोश जनजातियाँ और 198 विमुक्त जनजातियाँ हैं, जो पुलिस और न्यायिक प्रणालियों द्वारा निरंतर अलगाव और रूढ़िबद्धता के कारण औपनिवेशिक वर्गीकरण की विरासत का सामना कर रही हैं। विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, पूरे भारत में ऐसे 1,262 समुदाय हैं। हालाँकि अधिकांश विमुक्त जनजातियाँ अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में फैली हुई हैं, फिर भी कुछ किसी भी आरक्षण श्रेणी से बाहर हैं, जिससे सकारात्मक कार्रवाई के लाभों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
हाल के कानूनी घटनाक्रम
अक्टूबर 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदतन अपराधी वर्गीकरण के निरंतर उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि “एक पूरे समुदाय को न तो अतीत में एक आपराधिक जनजाति घोषित किया जाना चाहिए और न ही वर्तमान में एक आदतन अपराधी”। न्यायालय ने राज्यों से इन कानूनों की प्रासंगिकता और अनुप्रयोग की समीक्षा करने का आग्रह किया, खासकर जब ये पूरे समुदायों की रूपरेखा तैयार करने के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह हस्तक्षेप विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना किए जा रहे निरंतर भेदभाव की एक महत्वपूर्ण न्यायिक मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है।[17][27]
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईआरडी) ने 2007 में भारत से आदतन अपराधी अधिनियम को निरस्त करने का अनुरोध किया था, और इसे औपनिवेशिक युग के भेदभाव की निरंतरता के रूप में मान्यता दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विमुक्त जनजातियों का अध्ययन करने वाली विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू करने के महत्व पर बार-बार जोर दिया है, जिसमें भेदभावपूर्ण कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करना भी शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य आपराधिक जनजाति अधिनियम की विरासत को संबोधित करने के वैश्विक महत्व को उजागर करते हैं।[21][26][28]
सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ
समकालीन विमुक्त जनजातियाँ कई परस्पर जुड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं जो औपनिवेशिक वर्गीकरण के स्थायी प्रभाव को दर्शाती हैं। लगभग 11 करोड़ की आबादी के साथ, ये समुदाय प्रलेखित कलंक और उत्पीड़न से परे असाधारण स्तर के भेदभाव का सामना करते हैं। कई लोग सड़क पर सामान बेचने, घुमंतू मज़दूरी करने और छोटे-मोटे व्यापार जैसे पारंपरिक व्यवसायों में लगे रहते हैं, और अक्सर शिक्षा और औपचारिक रोज़गार के अवसरों तक सीमित पहुँच के कारण गरीबी में जीवन जीते हैं। भूमिहीनता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, और कई समुदाय भूमि अधिकारों के अभाव में फुटपाथों पर या असुरक्षित आवासों में रहने को मजबूर हैं।
सरकारी पहल और सुधार प्रयास
नीतिगत हस्तक्षेप
भारत सरकार ने विमुक्त जनजातियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। 2022 में शुरू की गई SEED योजना शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता पहलों के माध्यम से विमुक्त जनजातियों का समर्थन करती है। डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विमुक्त, विमुक्त और विमुक्त जनजातियों की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार खानाबदोश परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सृजित करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राज्य-स्तरीय पहल
विभिन्न राज्यों ने विशिष्ट विमुक्त समुदायों के लिए लक्षित कार्यक्रम लागू किए हैं। महाराष्ट्र विमुक्त जनजातियों के छात्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता और छात्रावास प्रदान करता है, जबकि तमिलनाडु नारिकुरवर और अन्य विमुक्त जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मध्य प्रदेश ने पारधी समुदाय के लिए निःशुल्क आवास और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए हैं, और गुजरात ने छारा समुदाय, जिन्हें पहले अपराधी माना जाता था, के लिए पुनर्वास कार्यक्रम विकसित किए हैं। ये राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप विभिन्न विमुक्त समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान को दर्शाते हैं।
संस्थागत तंत्र
राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) की स्थापना, विमुक्त जनजातियों के मुद्दों के अध्ययन और समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह आयोग उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ढाँचे के भीतर वर्गीकरण पर कार्य करता है और रेनके आयोग (2008) और इदाते आयोग (2014) सहित विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन कर चुका है। ये संस्थागत प्रयास नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन हेतु ढाँचा प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक विधान के सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक है, जो दर्शाता है कि कैसे कानूनी ढाँचों को जन्म और सामाजिक पहचान के आधार पर पूरे समुदायों पर व्यवस्थित रूप से अत्याचार करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है। इस अधिनियम में वंशानुगत अपराध की धारणा ने न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया और साथ ही नियंत्रण और सामाजिक इंजीनियरिंग के औपनिवेशिक प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति की। इसका प्रभाव कानूनी प्रतिबंधों से कहीं आगे तक फैला, जिससे स्थायी सामाजिक कलंक और आर्थिक हाशिए पर धकेले जाने का खतरा पैदा हुआ, जो आज भी लाखों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है।
स्वतंत्रता के सात दशक से भी अधिक समय बाद भी गैर-अधिसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव का जारी रहना औपनिवेशिक विरासत की गहरी संरचनात्मक प्रकृति और प्रणालीगत अन्याय को दूर करने में केवल औपचारिक कानूनी सुधारों की अपर्याप्तता को उजागर करता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम को आदतन अपराधी अधिनियम से प्रतिस्थापित करना दर्शाता है कि कैसे सुधार का दिखावा बनाए रखते हुए नए कानूनी ढाँचों के माध्यम से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को जारी रखा जा सकता है। विमुक्त जनजातियों के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियाँ—जिनमें पुलिस उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक हाशिए पर डालना और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव शामिल है—स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज पर औपनिवेशिक वर्गीकरण प्रणालियों के स्थायी प्रभाव को दर्शाती हैं।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदतन अपराधी कानूनों पर सवाल उठाने और उन्हें निरस्त करने की अंतर्राष्ट्रीय मांगों से व्यापक कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता का संकेत मिलता है। हालाँकि, आपराधिक जनजाति अधिनियम की विरासत से निपटने के लिए विधायी परिवर्तनों से कहीं अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण, पुलिसिंग प्रथाओं और संस्थागत ढाँचों में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है जो औपनिवेशिक युग के पूर्वाग्रहों को कायम रखते हैं। विमुक्त जनजातियों का सम्मान, समानता और न्याय के लिए संघर्ष संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है,